"शब्दों के जादूगर मजरुह सुल्तानपुरी"
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल
'मजरुह सुल्तानपुरी'
मजरुह सुल्तानपुरी एक ऐसा शब्दों का जादूगर, जिन्होंने ग़ज़लें, शायरी, गीतों को रचा. नायाब हर्फों का पूरा का पूरा नौ रंगों का संगीत, साहित्य को रचते हुए अपने नेपथ्य में चले गए. टूटे हुए दिलों को मरहम लगाते गीत. उदास शामों के नग्मे, उर्जावान सुबह को परिभाषित करते गीत. प्रेमी - प्रेमिका एक - दूसरे को आसमान लेकर आने वाले गीत. सामजिक सरोकार को दर्शाती हुई उनकी कलम की ताकत, बिना किसी संकोच, भय के मदमस्त होती सत्ता के सीने में चढ़कर उसके नाकाब उतारने का हुनर, मजरुह सुल्तानपुरी साहब को एक ऐसा क्रांतिकारी बनाती थी, जो सत्ता से टकराते हुए जेल की दीवारों में कैद हो गए. कभी समझौता नहीं किया, साहित्यकारों के चने खाकर ज़िन्दा रहने की बात को भी सच कर दिखाया.
मजरुह सुल्तानपुरी एक ऐसे शायर, गीतकार, जिनके गीत ज़ख्मी दिलों पर मरहम का काम करते थे. हिन्दी सिनेमा के ऐसे गीतकार जिन्होंने गीतकार बनने से पहले रोजमर्रा की ज़िन्दगी जीने के लिए युनानी हकीम की शिक्षा ली, और ज़ख्मी दिलों पर अपनी रूहानी शायरी का मरहम लगाया. उनके संगीत में बांसुरी की धुन, जीवन का सार गांव की इंसानी जिंदगियां झलकती हैं. मजरुह के गीतों में एक तरफ सबकुछ बहा ले जाने वाला दर्द का सागर उमड़ रहा होता था. वहीँ मजरुह के गीतों में ज़िन्दगी से हार न मानने वाली दिलेरी भी होती थी. जिन्हें ज़िन्दगी के खोए रंगों को उकेरने में पूर्ण स्वामित्व था. तहज़ीब, नजाकत, नफासत, उनकी लेखनी का श्रंगार होते थे. मजरुह सुल्तानपुरी ऐसे अजूबे गीतकार जो गोल्डन एरा के पहले से ही अंतिम नब्बे के दशक तक सक्रिय रहे, जिन्होंने के एल सहगल से लेकर, देव - राज - दिलीप से लेकर शाहरुख, सलमान, आमिर को सुपरस्टार बनाया. हिन्दी सिनेमा में 50 से 70 के दशक के बीच का युग को गोल्डन एरा कहा जाता है. इससे पहले ही 30 से 40 के दशक में ही हिन्दी सिनेमा के साथ संगीत को पर्याय बनाने के लिए पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया. उनमे सबसे ज्यादा योगदान केदार शर्मा, कवि प्रदीप, डी एन मधोक आदि प्रमुख नाम थे. ठीक इनके बाद कैफ़ी आज़मी, कमर जलालाबादी, राजेन्द्र किशन आदि दूरदर्शी गीतकार हिन्दी सिनेमा के संगीत को स्वर्णिम युग में ले जा रहे थे.
समूचे देश में आजादी की लड़ाई, साम्यवादी, वामपंथियों का अपना - अपना सामजिक गुट बन रहा था. वहीँ गांधी का समाज पर प्रभाव एवं नेहरू की अपनी लोकप्रियता तो बुलंदियों पर थी. ऐसे ही बदलते हुए समाज के साथ हिन्दी सिनेमा एतिहासिक फ़िल्में बना रहा था. ऐसे ही बदलते माहौल में शायर मजरुह सुल्तानपुरी ने फिल्म शाहजहां से अपना बतौर गीतकार अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया. इस सुपरहिट फिल्म में गायक एवं अभिनेता के एल सहगल को सुपरस्टारडम के आसमान पर पहुंचा दिया था. आज भी सिने प्रेमी के एल सहगल को याद मजरुह सुल्तानपुरी के गीतों के लिए याद करते हैं.
'ग़म दिये मुस्तक़िल, इतना नाज़ुक है दिल,
ये न जाना हाय हाय ये ज़ालिम ज़माना
वही के एल सहगल का दूसरा गीत
' जब दिल ही टूट गय हम जी के क्या करेंगे
उलफत का दिया हमने इस दिल में जलाया था
उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था
इक भेदी लूट गया '
मजरुह सुल्तानपुरी जिस बदलते हुए भारत में हिन्दी सिनेमा में आए थे, उस समय हिन्दी सिनेमा के गीतों में भाषायी प्रयोग होने लगे थे. हिन्दी सिनेमा में गीत फ़िल्मों के जरूरी अंग बन चुके थे. तब तक हिन्दी सिनेमा के गीत लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे थे. तब तक आम लोगों के सरोकार से जुड़ते हुए गीतों की विरासत मजरुह सुल्तानपुरी पचास साल तक समय - समय पर बदलते हुए परिवेश के साथ अपने अधिकारों को कांधे पर उठाए रहे. आसान नहीं था, मजरुह सुल्तानपुरी बनना.
हमेशा से कलम की यात्रा सबसे ज्यादा संघर्षशील, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा बहुमुखी सभी विधा का मार्गदर्शन करने वाली विधा रही है. वहीं कला के साथ संगीत, साहित्य का जुड़ जाना हमेशा से ताकत का अनूठा मापदंड रहा है. साहित्य की भूख - प्यास, धूप-छांव आम जनमानस के सरोकार से जुड़ी रही थी , इसलिए हिन्दी सिनेमा के गीतों को गागर में सागर भरने वाली विधा माना जाता है. जनसरोकारों से जुड़े रहने के कारण यह विधा ताकतवर है, जब भी इसकी धारा मुड़ेगी न साहित्य रहेगा, न ताकत रहेगी, न बचेगा संगीत न रह जाएगी वो विधा जिसके प्रमुख सूत्रधार मजरुह सुल्तानपुरी साहब भी थे. गीतकारों को अपने गीतों में प्रेम, रोमांस, ट्रेजडी, हास्य, के साथ देश प्रेम छायावाद, भजन, कैबरे, होली, दिवाली, जैसे गीतों के साथ जीवन दर्शन और दार्शनिक विचार का अनूठा संगम रचना एवं चंद मिनटों में लोगों को जोड़ देना एक अनूठी विधा है. हिन्दी सिनेमा में सौ सालों से अधिक गीतों के संगीत का इतिहास उसकी अपनी स्वीकार्यता हमेशा से ही हमें अपने संवेदनशील विचारो से हमारे जीवन को सींच रही है.
सामजिक संवेदनशीलता को सिंचित करती हुई गीतों की विधा के पुरोधा मजरुह सुल्तानपुरी साहब को जब 1993 में
हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े पुरूस्कार से सम्मानित किया जाना था, तो उन्होंने सम्मान लेने से मना कर दिया. जब कि दादा साहब फाल्के पुरूस्कार प्राप्त करने वाले मजरुह सुल्तानपुरी पहले गीतकार थे. मजरुह सुल्तानपुरी साहब ने कहा "मेरा जीवन सम्मान लेने के लिए नहीं हुआ है. मेरा काम सामाजिक चेतना का प्रसार करना है. दरअसल मैं सम्मान ले भी लूँ, लेकिन अब मैं नहीं ले सकता क्यों कि जिन फिरकापरस्तों की विचारधारा के विरुद्ध मैं जीवन भर लड़ता रहा उस हाथों से सम्मान लेना उतने सारे जुल्मों को सही ठहराने जैसा है". यह बात उन्होंने महाराष्ट्र के सर्वमान्य नेता बालासाहब ठाकरे के लिए कहा था, क्योंकि यह सम्मान बालासाहब ठाकरे के हाथो से दिया जाना था. यह वो दौर था जब बालासाहब ठाकरे के खिलाफ़ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी, शायद आज भी नहीं है.
भागती हुई मुंबई भला किसके लिए रुकी है, वो चल पड़ी थी.
"मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर
लोग साथ आते गए कारवाँ बनता गया"
"तुझे न माने कोई तुझे इससे क्या मजरुह
चल अपनी राह भटकने दे नुक्ता चीनो को
ये दोनों शेर मजरुह सुल्तानपुरी की सिनेमाई यात्रा एवं साहित्यक दुनिया को बयां करते हैं. मजरुह साहब ने शायरी को एवं गीतों का दोनों को अलग - अलग मुकाम तक पहुंचाया. कभी भी दोनों को मिश्रित नहीं होने दिया. हिन्दी सिनेमा में मजरुह सुल्तानपुरी का कारवाँ बनना तो दूर की बात है, उन्होंने हिन्दी सिनेमा के साथ चलने से ही मना कर दिया था. 1945 में मजरुह सुल्तानपुरी एक मुशायरे में मुंबई पहुंचे. मुशायरे में फ़िल्मकार के आर कारदार ने मजरुह सुल्तानपुरी को सुना, वो मजरुह सुल्तानपुरी के शब्दों के मुरीद हो गए थे. उन्होंने मजरुह सुल्तानपुरी को अपनी फ़िल्मों में गीत लिखने को कहा, लेकिन मजरुह सुल्तानपुरी को फ़िल्मों में लिखना पसंद नहीं था, अतः के आर कारदार ने मजरुह सुल्तानपुरी के गुरु जिगर मुरादाबादी को समझाने के लिए कहा, फ़िल्मकार ने कहा कि उन्हें समझाईए की जिंदगी में शोहरत ही सबकुछ नहीं होती जीवन यापन के लिए पैसे की जरूरत भी होती है. जिगर मुरादाबादी को भी मजरुह ने मना कर दिया, जैसे गीतकार शैलेन्द्र ने राजकपूर को मना कर दिया था. गुरु ने जीवन की सच्चाइयों को स्वीकारने के लिए कहा अंततः मजरुह सुल्तानपुरी लिखने के लिए मान गए. फिर हिन्दी सिनेमा में शुरू हुआ मजरुह सुल्तानपुरी का सुनहरा दौर जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता था.
चालीस के दशक में बहुत कुछ बदल रहा था, आजादी का जश्न एक तरफ वहीँ देश बंटवारे की आग में जल रहा था. वहीँ हिन्दी सिनेमा अपने गोल्डन एरा में प्रवेश कर चुका था. मजरुह सुल्तानपुरी यूँ तो गीत लिख ही रहे थे, 1949 महबूब खान ने फिल्म अंदाज़ बनाया उसके गीतों को लिखने की जिम्मेदारी मजरुह सुल्तानपुरी के पास थी. फिल्म के साथ साथ मजरुह सुल्तानपुरी हिट हो गए थे. फिल्म को सफ़लता तो मिली.
वहीँ तत्कालीन सत्ता की खिलाफ़त ने उन्हें जेल पहुंचा दिया था. हर युग हर समय में सत्ता का चेहरा एक जैसा ही होता है, वह अपनी आलोचना नहीं सह सकती थी, सत्ता के विरुद्ध जाने वाले का दमन कर दिया जाता है. वही मजरुह सुल्तानपुरी के साथ हुआ. आज़ाद भारत की पहली सरकार का प्रमुख चेहरा रहे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की दोहरी नीतियों के खिलाफ सत्ता की छाती पर चढ़कर उसके काले नकाब उतार दिए थे. मजरुह सुल्तानपुरी की लेखनी से नेहरू की सत्ता ने उन्हें जेल में डाल दिया. उन्होंने पंडित नेहरू के चेहरे के नकाब को उतारते हुए लिखा था. आज के दौर में सत्ता के साथ कदमताल करते गीतकारों को देखकर मजरुह सुल्तानपुरी की आत्मा जहां भी होंगी कचोटती होगी, कि मैंने ऐसी लकीरें तो नहीं खींची थी. पंडित नेहरू के लिए मजरुह सुल्तानपुरी ने क्या लिखा था कि जेल जाना पड़ा.
"मन में ज़हर डॉलर के बसा के
फिरती है भारत की अहिंसा
खादी की केंचुल को पहनकर
ये केंचुल लहराने न पाए
ये भी है हिटलर का चेला
मार लो साथी जाने न पाए
कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू
मजरुह सुल्तानपुरी की तरबियत एवं मिजाज़ ऐसा ही था. चूंकि नेहरू भी सेकुलर छवि के मालिक थे, उन्होंने मजरुह सुल्तानपुरी से कहा कि माफी मांग लीजिए, लेकिन मजरुह सुल्तानपुरी साहब ने जेल में रहना ही मुनासिब समझा. मजरुह साहब के जेल जाने के कारण उनकी घर की आर्थिक हालत खराब हो गई थी . हर किसी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कमाया होता कि मुश्किल के दिनों में वो काम आता है. मजरुह सुल्तानपुरी साहब की मदद के लिए ग्रेट शो मैन राज कपूर साहब ने मजरुह सुल्तानपुरी से गुजारिश की, कहा मजरुह साहब मैं आपके बच्चों की हालत ऐसी नहीं देख सकता महान इंसान के घरवालों को इस हालात में देखना मुनासिब नहीं है, लेकिन मजरुह सुल्तानपुरी तो खुद्दार इंसान थे, उन्होंने मना कर दिया था कि राज साहब में फ्री में मदद नहीं ले सकता मेरी ग़ैरत इसके लिए हाँ नहीं कहती. तब राज कपूर साहब ने मजरुह सुल्तानपुरी साहब की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी फिल्म में गीत लिखने के लिए गुजारिश किया. आख़िरकार गीतकार गीत लिखने के लिए मान गए. राजकपूर ने मजरुह सुल्तानपुरी को गीत लिखने का मेहनताना एक हजार रुपये दिया, उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी. मजरुह सुल्तानपुरी ने जेल में रहते हुए एक कालजयी गीत लिखकर दिया. राज कपूर ने वो गीत बहुत सालो तक संजोकर रखा वह गीत जीवन की सच्चाइयों को समेटे हुए था.
गीत के बोल थे
"एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल
जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल" इस गीत को राज कपूर ने अपनी फिल्म धरम-करम में उपयोग किया. यह गीत हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम रखता है.
जेल से बाहर आने के बाद शुरुआती पचास के दशक में हिन्दी सिनेमा में राज करने वाली गीतकारों की चौकड़ी गीतों के राजकुमार कविराज शैलेन्द्र, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूंनी, खुद मजरुह सुल्तानपुरी शामिल थे. आजादी के बाद पचास के दशक में हिन्दी सिनेमा गंभीर सामजिक प्रयोग करते हुए सिनेमा नए आयाम गढ रहा था. जिसमें संगीत एवं फ़िल्मों में उसकी लोकप्रियता के लिए आवश्यक था, किसी नई शब्दावली वाले रचनाकार का जो गीतों के लिहाज से कुछ नया हो, शब्दों का ऐसा भाव जो दिल तक पंहुचे और जुबान पर आ जाए. मजरुह सुल्तानपुरी ने अपनी कलम से गीतों को रचा था. मजरुह सुल्तानपुरी साहब ने जो गीत लिखे वॊ अपने समय के लिए तो थे ही साथ ही हमेशा के लिए प्रासंगिक रहेंगे. उनके गीत आने वाली पीढ़ी के गीतकारों के लिए पूरा का पूरा सिलेबस है. मजरुह सुल्तानपुरी ने हर संगीतकार, प्रत्येक अभिनेता के लिए गीत लिखे थे. उनके गीतों में ग़ज़ब का प्रवाह होता था, जिसके साथ पीढ़ियां जुड़ती चली गईं. मजरुह सुल्तानपुरी अपने गीतों में समय समय पर जो परिवेश बदल रहा था उसके हिसाब से खुद भी बदलाव कर रहे थे.
गीतकारों की अपनी मर्यादा होती है, संगीत एवं गीतों में बंदिशें होती हैं. किस धुन पर कितनी मात्रा होना चाहिए. गीत लिखते हुए केवल भाषा सहित कई सीमाएं होती हैं. गाने की धुन परिस्थिति के हिसाब से संगीत के मीटर पर चलना बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है. शब्दों में गहराई के साथ सरलता बहुत आवश्यक है. तीन चार मिनट के गीत में इतनी सारी खूबियां होना गागर में सागर भरने वाला है. इसके साथ ही फिल्म के निर्माता / निर्देशक की पसंद के साथ - साथ हीरो की पसंद का भी ख्याल रखना होता है. वहीं गीतों के व्यापारीकरण का भी हित ध्यान में रखते हुए लिखना होता है. फिल्म के गीतों में जिसे सिनेमाई भाषा में हिट न. होना जरूरी होता है. जिसका होना फिल्म हिट होने की गारंटी होता है. हर बदलते हुए समय के साथ अपने गीतों में मजरुह सुल्तानपुरी ने बहुत ही दूरदर्शी अंदाज़ पेश किया. मजरुह सुल्तानपुरी के हिट गानों का कारवाँ नब्बे के दशक में भी बुलंदियों पर रहा. नब्बे के दशक में समीर - अंजान का दौर शुरू हो चुका था. उनके बाद इरर्शाद कामिल, प्रसून जोशी, अमिताभ भट्टाचार्य, जैसे प्रतिभावान गीतकार जो इस विधा को आगे बढ़ा रहे थे. इन सभी की मौजूदगी में मजरुह सुल्तानपुरी पूरी तरह से आधुनिक हो चुके थे. गानों के रीमिक्स में गानों में हेर-फेर कर के बेचा जा रहा था, तब भी मजरुह सुल्तानपुरी के गीत प्रासंगिक रहे. मजरुह सुल्तानपुरी बदलते हुए इस युग में जो संगीत दिवालियापन हो चुका था, मजरुह सुल्तानपुरी ने उसकी कड़ी शब्दों में आलोचना की. मजरुह सुल्तानपुरी ने कहा " आदमी में फ़ितरत में ईमानदारी होती है यह मूल बात है, बेईमानी बनाई हुई बात है, आज के दौर में हमारे गाने लोग बिना इजाजत उपयोग कर लेते हैं, उस को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारी दिल से की गई मेहनत में जिसको हमने सामजिक सरोकार के लिए रचा था, उसे व्यापारीकरण के लिए फूहड़ता का मिश्रण सहन नहीं होता. हर एक सूर्य जब उगता है तो उसको अस्त होना होता है. हिन्दी सिनेमा में सबसे अनोखे गीतकार सामाजिक सरोकार की शायरी लिखने वाले शायर 24 मई सन 2000 को इस फानी दुनिया से रुख़सत कर गए. जब तक हिन्दी सिनेमा है तब तक जिंदा रहेंगे. हर टूटे हुए दिल से फ़ूट पड़ेंगे, वहीँ ज़ख्मी दिलों में मरहम लगाते रहेंगे, वहीँ सामजिक चेतना के प्रसार के लिए वो हमेशा याद आएंगे. जब जब सत्ता से कोई कलमकार टकराते हुए भिड़ेगा तब तक मजरुह सुल्तानपुरी याद आएंगे....जब तक मानवीय जीवन है तब तक मजरुह सुल्तानपुरी साहब जिंदा रहेगे.
दिलीप कुमार









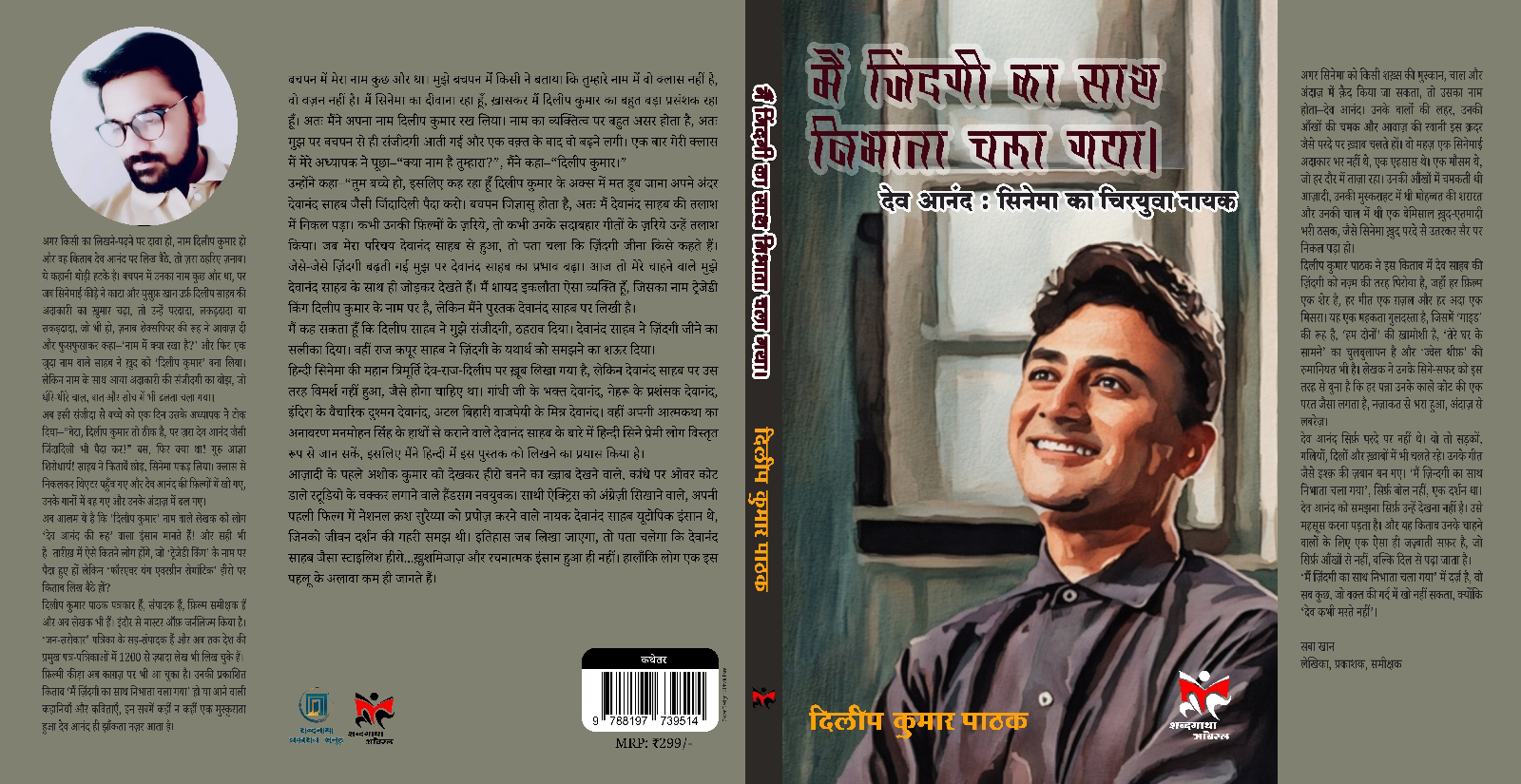


Comments
Post a Comment