"शांति स्वस्थ्य समाज़ की आवश्यकता है"
शांति स्वस्थ्य समाज़ की आवश्यकता है"
शांति वाद - प्रतिवाद का विषय नहीं है, जिस पर विमर्श किया जाए, शांति स्वस्थ, समृद्ध समाज की आवश्यकता है. शांति ही वो रास्ता है जो प्रगति की ओर ले जाता है, वैसे भी युद्ध, हिंसा, घृणा से चित्कार के अलावा कुछ नहीं निकलता. युद्ध समाज एवं राष्ट्र को सीधा विनाश की ओर ले जाता है, अतः जब तक सारे मार्ग बंद न हो जाएं तब तक शांति के अतिरिक्त कोई समृद्ध रास्ता है नहीं है.
आज हमारे समाज में भी नफ़रत पंख फैला रही है. सीरिया, अफगानिस्तान, फलस्तीन, रसिया, यूक्रेन से पहले हमें अपने राष्ट्र में फैल रही घृणा, नफ़रत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना होगा.. अब कई लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल महाभारत का बिगुल फूंकने वाले के रूप में प्रचारित करते हैं तो उन्हें बताना होगा कि युद्ध के बारे में भगवान श्री कृष्ण के विचार ऐसे नहीं हैं जैसा आधुनिक युग अपने हिसाब से गढ लेता है. आज श्री कृष्ण को महाभारत कराने वाले नायक के रूप में याद किया जाता है, कितना दुर्भाग्य है लोग अपने आराध्य भगवान को ढंग से जानते ही नहीं. जबकि देखा जाए तो महाभारत में दोनों पक्षों में केवल केवल एक श्री कृष्ण ही थे, जो शांति की बात कर रहे थे, अन्यथा सारे के सारे युद्ध की अग्नि में कूदने के लिए आतुर थे. इसलिए नहीं कि श्रीकृष्ण द्रोपदी के अपमान को भूल गए थे, अपितु वे आम जनमानस को समझाना चाहते थे कि युद्ध आखिरी विकल्प होता है. श्री कृष्ण ने भीम अर्जुन को कहा - "ज़न कल्याण से ज़रूरी तुम्हारी प्रतिज्ञाएं नहीं हैं. अगर युद्घ रुक जाता है तो रुक जाना चाहिए. युद्घ के आँगन में स्वस्थ्य समाज़ का निर्माण नहीं हो सकता. द्रोपदी से श्रीकृष्ण कहते हैं - " शांति कोई विकल्प नहीं है आवश्यकता है. ग़र शांति मिलती है तो समझो सस्ती है. और जनकल्याण के लिए युद्घ कोई रास्ता नहीं होता. हस्तिनापुर एक सागर है, और तुम एक बूंद...कोई भी राजा एवं उसकी महत्त्वाकांक्षा किसी जनमानस से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती. और युद्द किसी भी राजा की महत्वाकांक्षा की उपज होती है.
भारत ने हमेशा शांति की बात की है, भारत ने हमेशा शांति की बात इसलिए नहीं कि है कि भारत ने युद्घ नहीं लड़े, बल्कि भारत इसलिए शांति की बात करता है कि भारत को युद्घ की विभीषिका का मर्म पता है. भारत हज़ारों युद्ध जी चुका है, भारत हज़ारों युद्धों का गवाह है. भारत ने वो खूनी तांडव देखे हैं अतः भारत का उतरदायित्व बढ़ जाता है कि वो दुनिया को शांति की कीमत समझाए. और भारत ने हमेशा से ही शांति का मार्ग अपनाया है. आज हम अपने देश में एक - दूसरे से असहमत हो सकते हैं लेकिन हमें पता है कि असहमतियों के बीच कड़वाहट नहीं होनी चाहिए. भारत ने इतिहास में असहमतियों के बीच कड़वाहट का वो दौर जिया है. दो सौ साल की लम्बी गुलामी झेलते हुए भारत के हमारे एक महान पूर्वज महात्मा गांधी ने शांति, अहिंसा की बात की थी. ऐसा नहीं है कि गांधी जी की एक हुंकार पर करोड़ों लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गांधी जी को पता था कि युद्ध केवल एक सैनिक एक नागरिक नहीं लड़ता, बल्कि युद्ध एक बेटा, बाप, भाई, पति, युद्घ लड़ता है, जिसके साथ कंधे से कंधा मिलकर माँ, पत्नी, बेटी, बहिन भी युद्ध में भाग लेती है. युद्ध की विभीषिका आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है. युद्ध नफ़रत से शुरू होता ज़रूर हैं लेकिन युद्घ मुहब्बत की उम्मीद पर खत्म होता है, अतः मुहब्बत का रास्ता कभी भी नहीं त्यागना चाहिए.
महात्मा गांधी अहिंसा, शांति के ऐसे दूत थे जो अपने आचरण से पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिखाते हैं. ये सोचने की बात नहीं है कि आज गांधी जी होते तो क्या करते. बापू अहिंसा त्याग कर अधिकांश युद्घ के मार्ग पर चल पड़ी दुनिया के विरुद्ध खड़े दिखाई देते. आज गांधी जी अनशन पर बैठे हुए दुनिया को शांति की स्थापना का मार्ग बताते, क्योंकि शांति ही प्रगति पथ है. गांधी जी का सबसे प्रमुख जीवन का मंत्र अहिंसा था और वे आज भी अहिंसा के महत्व का प्रचार कर रहे होते और अहिंसा की प्रासंगिकता लोगों को समझा रहे होते. उन्होंने अपने जीवन में अग्रेजों के अत्याचार को देखा सहा और उनके शक्तिशाली होने के बाद भी उनसे निपटने के लिए अपने निजी जीवन और धार्मिक मूल्यों को लागू किया और सत्य और अहिंसा का रास्ता निकाला. अहिंसा अर्थ हिंसा ना करना होता है, किसी की हत्या ना करना या किसी को कष्ट ना पहुंचाना होता है. व्यापक अर्थ में अहिंसा को किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वनऔर वाणी से नुकसान ना पहुंचाना और कर्म से किसी भी प्राणी की हिंसा का नहीं करना ही अहिंसा है. केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अहिंसक हो सकता है, क्योंकि उसमें चेतना होती है. अहिंसा ही समस्त शक्तियों में सबसे शक्तिशाली है. बापू कहते थे - "कमजोर नहीं बल्कि सही अर्थों में शक्तिशाली ही क्षमा कर सकता है और जो हिंसा करता है वास्तव में वह कमजोर ही है. कभी - कभार क्रोध को पानी की भांति पी जाना चाहिए. क्षमा धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है, क्षमा ही ब्रम्ह है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा तप है, क्षमा शक्तिशाली का बल है. अतः क्षमा का मार्ग कभी नहीं त्यागना चाहिए. भारत को दो सदी से अधिक समय तक गुलाम बनाकर रखने वाला ब्रिटेन अपनी संसद में गाँधी जी की प्रतिमा बनाकर गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पर चलने की कसमे खाता है, यही गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत है
श्री कृष्ण, बुद्ध, गांधी जी हर किसी ने शांति को परम आवश्यक बताया है. आज जब दुनिया के हुक्मरानों को युद्घ की सनक रहती है.. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी दुनिया में युद्ध हुए जिनकी निशानियाँ आज भी मिटी नहीं है वो रहकर पूरी मनुष्यता पर कलंकित होने का आरोप लगाती हैं.
नफ़रत की रोटी खाने वालों को साहिर लुधियानवी के इस शे'र पर ध्यान देना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है
--------- जंग तो ख़ुद ही एक मसअला
जंग क्या मसअलों का हल देगी
बशीर बद्र साहब जैसे कलमकार ने दुनिया में बढ़ रही नफ़रत पर इस कलाम के ज़रिए अपील की थी-
----------------सात संदूक़ों में भर कर दफ़्न कर दो नफ़रतें
आज इंसाँ को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत
आज के आधुनिक दौर में यूनाइटेड नेशन जब पूरी दुनिया के बॉस होने का दावा करता है, उसकी दुनिया में कितनी सुनी जाती है, वो विमर्श का विषय है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कभी भी शांति को विकल्प नहीं कहा बल्कि उसने हमेशा शांति को आवश्यकता के रूप में देखा है. इसलिए ही यूनाइटेड नेशन ने 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में घोषित कर रखा है. विश्व शांति दिवस' या 'अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस' पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 सितम्बर को मनाया जाता है. शांति का संदेश दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत और खेल जगत की विश्वविख्यात हस्तियों को शांतिदूत भी नियुक्त कर रखा है.
शांति सभी को प्यारी होती है, इसकी खोज में मनुष्य अपना अधिकांश जीवन न्यौछावर कर देता है, परन्तु कितना अफसोसजनक है कि आधुनिक होती पीढ़ियां शांति छोड़कर साम्राज्यवाद की ओर बढ़ रही हैं. भला ऐसे कैसे शांति स्थापित हो सकती है? आज इंसान दिन-प्रतिदिन शांति से दूर होता जा रहा है. आज चारों तरफ़ फैले बाज़ारवाद ने शांति को व्यक्ति से और भी दूर कर दिया है. पृथ्वी, समुद्र, अंतरिक्ष सभी जगह क़ब्ज़ा कर लेने वाली सोच दुनिया को उन्माद की ओर ले जा रही है. स्वार्थ और घृणा ने मानव समाज को विखंडित कर दिया है. यूँ तो 'विश्व शांति' का संदेश हर युग और हर दौर में दिया गया है, लेकिन इसको अमल में लाने वालों की संख्या उन्मादी लोगों से बहुत ज़्यादा रही है लेकिन समय - समय पर कुछ महात्वाकांक्षी सोच के प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण शांति अपभंग होती रही है.
फिर भी भारत ने शांति का क्षमा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जब इंग्लैंड गए तो उनकी मुलाकात ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल से हुई. पिछली बातों को याद करते हुए चर्चिल ने जब उनसे पूछा - "आपने अंग्रेजों के शासन में कितने वर्ष जेल में बिताए? नेहरू का जवाब था कि 10 वर्ष.. चर्चिल ने पुन: सवाल किया -" तब तो अपने साथ किए गए व्यवहार के प्रति आप हमसे घृणा करते होंगे? पंडित नेहरू ने तपाक से उत्तर दिया - "बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमने एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम किया है, जिसने हमें दो बातें सिखाई, एक किसी से डरो मत और दूसरा, किसी से घृणा मत करो.. हम उस समय आपसे डरते नहीं थे और आज घृणा भी नहीं करते.. दरअसल नेहरू जी ने महात्मा गांधी की बात की थी. यही कारण है कि पण्डित नेहरू ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पाँच मूल मंत्र दिए थे, इन्हें ही 'पंचशील के सिद्धांत' कहा जाता है. जनकल्याण एवं विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में पारस्परिक सहयोग के पाँच आधारभूत सिद्धांत हैं, जो कुछ इस तरह हैं,
एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना...
एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना..
एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना..
समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना..
शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना..
माना जाता है अगर विश्व उपरोक्त पाँच बिंदुओं पर अमल करे तो हर तरफ़ चैन और अमन का ही वास होगा..
आज प्रत्येक व्यक्ति को गहराई से सोचना होगा, कि ये दौर बड़ा सस्ता है. तब ही सोचना होगा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है. मानव कल्याण की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं. भाषा, संस्कृति, पहनावे भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विश्व के कल्याण का मार्ग एक ही है. मनुष्य को नफरत का मार्ग छोड़कर प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए. शांति के महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया कि हर 21 सितम्बर को 'विश्व शांति दिवस' मनाया जाएगा. इस सदी में विश्व में फैली अशांति और हिंसा को देखते हुए हाल के सालों में शांति कायम करना मुश्किल ही लगता है, किंतु उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही वह दिन आएगा, जब हर तरफ शांति ही शांति होगी... वैसे भी शांति, क्षमा, का मार्ग कभी भी नहीं त्यागना चाहिए.
दिलीप कुमार पाठक

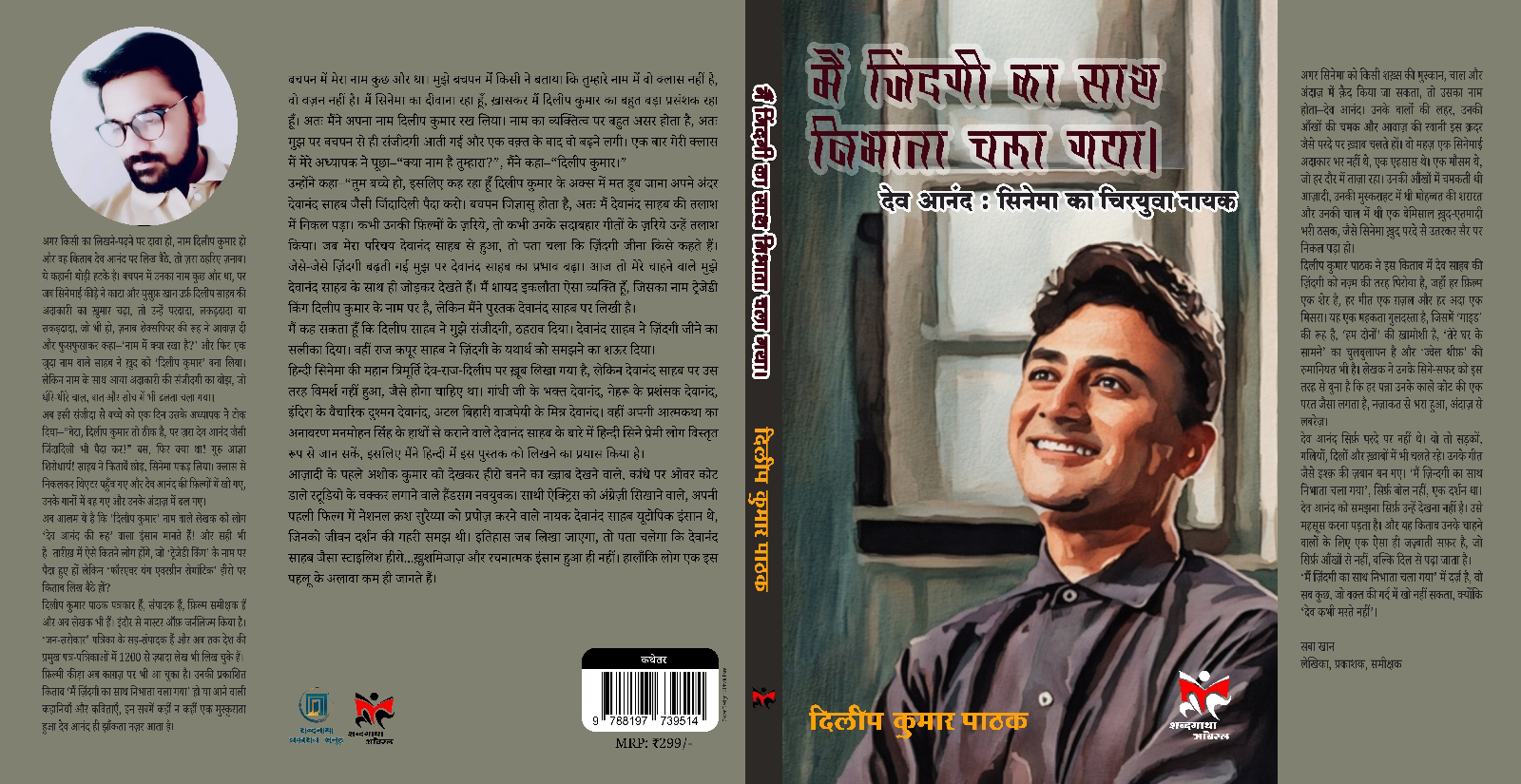


Comments
Post a Comment