हिन्दी भाषियों की जुबान से दूर होती जा रही है वैश्विक भाषा हिन्दी
हिन्दी भाषियों की जुबान से दूर होती जा रही है वैश्विक भाषा हिन्दी
--------------------------------------------------------------------------
हमें विविधतापूर्ण जीवन जीने की कल्पना करना चाहिए, और हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को संकीर्ण तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए. दुनिया विविधतापूर्ण ही अच्छी लगती है. लेकिन हमें अपनी विरासत को सहेजना चाहिए, और यह हमारा उत्तरदायित्व होता है. लेकिन एक दुःखद सत्य यह भी है. हम सहेजने के मामले में दुनिया के सबसे फिसड्डी लोगों में शुमार हैं. आजतक हम न तो ढंग से अपनी धरोहरें सम्भाल पाए हैं और न ही अपनी राजभाषा हिन्दी...आज 14 अगस्त हिन्दी दिवस है तो जानना ज़रूरी है कि हमारी राजभाषा हिन्दी किस मुकाम पर है. सच तो यह है कि आज हमारी राजभाषा हिन्दी लोगों की जुबान से दिन प्रति दिन दूर होती जा रही है, हमारे देश एवं मूल हिन्दी वासियों के लिए शर्मनाक तो है ही साथ ही चिंता का विषय भी है. हम सब भले ही उदारवाद के नाम पर अपनी भाषा को महत्त्व न दें लेकिन हमारी भाषा हमारे अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होती है. पूरी दुनिया अपनी - अपनी भाषाओं को बड़ी सहजता और स्वाभाविक रूप से लेते हैं, लेकिन हम भारतीय ही एक अपवाद हैं, जो अपनी भाषा के प्रति दोयम दर्जे की सोच रखते हैं. हिन्दी लिखने - बोलने के कारण बहुतेरे लोग दूसरे लोगों को चिढ़ाते हुए असहज कर देते हैं, ये हमारे समाज की एक सच्चाई है कि हम अपनी भाषा बोलने वाले को पिछड़ा हुआ मानकर फब्तियां कसते हैं. जबकि किसी भी भाषा पर अधिकार रखने के पीछे एक सीख और एक समर्पण होता है. गहराई से देखा जाए तो कोई भी भाषा ख़राब, कमज़ोर नहीं होतीं, सारी की सारी भाषाएं विकराल रूप में होती हैं, वहीँ समझ आने के बाद कुछ अपनी लगने लगती हैं. समझ नहीं आने पर विकराल तो होती ही हैं. हालांकि यह भी सच है कि भाषाओं में सुधारों की गुंजाईश होती है, कोई भी भाषा परिपूर्ण नहीं होती है. समय - समय पर विद्वानों ने भाषाओ में सुधार भी किए हैं.
अब गूगल से लेकर दुनिया की तमाम बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हिंदी को तरजीह दे रही हैं. इनका मकसद भले ही उपभोक्ता हो पर उससे कहीं न कहीं हिंदी एक वैश्विक ताकत के तौर पर तो मजबूती पा रही है. यही नहीं 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के मतदान पर्ची पर पहली बार हिंदी में मतदाताओं को धन्यवाद का उल्लेख किया गया था. अमेरिका के चुनावी इतिहास में पहली बार अन्य भाषाओं के साथ हिंदी ने अपनी जगह बनाई. यह एक भाषा के बढ़ते दायरे का प्रतीक तो है ही इसके साथ वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्वीकार्यता का प्रमाण भी है.आज दुनिया में लगभग सभी देशों में हिंदी बोलने वालों की संख्या एक अरब तीस करोड़ के पार पहुंच चुकी है जो कि दुनिया में बोली जाने वाली किसी भी भाषा से अधिक है. हिंदी की वैश्विक स्वीकार्यता का बड़ा कारण भारत का डिजिटल माध्यमों के जरिए भाषा का विस्तार और उसके फलस्वरूप उपभोक्ता बाजार, हिंदी सिनेमा और भारतीय संस्कृति को जानने-समझने की ललक है. इस ललक में डिजिटल माध्यमों के मार्फ़त हिंदी की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है. माइक्रोसॉफ्ट के जरिए हिंदी का विकास और सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग आदि के जरिए हिंदी की वैश्विक उपस्थिति ने भारत के प्रति लोगों की जिज्ञासा को बढाया और वैश्विक स्तर पर हिंदी को नई पहचान दी. दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कई अवसरों पर अमरीकियों को हिन्दी सीखने के लिये सचेत करते हुए कह चुके हैं कि- "हिन्दी सीखे बिना भविष्य में काम नहीं चलेगा".. वैसे भी यह सलाह अकारण ही नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा व्यपारिक गढ़ है.
हालांकि अमेरिका में क्या हुआ इस पर गर्व करने की बजाय अपने देश में सुधार की आवश्यकता है. हमारे देश में कम से कम लोगों को हिन्दी बोलने के लिए प्रयास करना ही चाहिए, जिससे हमारी भाषा खत्म न हो अपितु लोगों के अभिव्यक्ति का माध्यम बनी रहे. हमारी जीवन-शैली में अहम भूमिका निभाने वाली हमारी राजभाषा दिन प्रति दिन अपने ही मुल्क में नकारी जाती है. इससे इंकार नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चों को विविध भाषाओ में शिक्षा देना भी हमारा दायित्व होता है. जो बच्चा जितनी भाषाएं समझेगा, लिखेगा ,बोलेगा उतना ही बोलने में दक्ष होगा. भाषाओ के मामले में हमें उदारवादी होना चाहिए, जिससे हम कहीं भी चले जाएं लोगों के साथ जुड़ पाएं. हिन्दी भाषा हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हैं लेकिन बदलते दौर में हिन्दी में सिर्फ़ गिरावट आई है. अब हमें हिन्दी के प्रति थोड़ा और ज़्यादा जागरूक होने और जागरूक करने की दरकार है. हिन्दी प्रकृति से यह उदार ग्रहणशील, सहिष्णु और भारत की राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका है. इस दिन विभिन्न शासकीय, अशासकीय कार्यालयों, शिक्षा संस्थाओं आदि में विविध गोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रतियोगिताओं तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है. कहीं-कहीं 'हिन्दी पखवाडा' तथा 'राष्ट्रभाषा सप्ताह' इत्यादि भी मनाये जाते हैं. विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध भाषा होने के साथ ही हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, अतः इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसे आयोजन स्वाभाविक हैं. परन्तु, दुःख का विषय यह है कि समय के साथ-साथ ये आयोजन केवल औपचारिकता मात्र बनते जा रहे.
अतः हम जब हिन्दी पर जागरुकता के लिए कार्यक्रम, संगोष्ठी करें लोगों को प्रेरित करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें संयम नहीं खोना है, बदलते हुए दौर में हिन्दी भाषियों में एक कट्टरता का भाव देखा गया है. हमें अपनी भाषा और भाषाविदों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और कृतज्ञता का भाव भी रखना चाहिए, लेकिन कई बार हमारे विद्वान संयम खो बैठते हैं, और अन्य भाषाओं के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं, यह कट्टरवाद खतरनाक तो है ही साथ ही उदारवादियों में एक अलग ही खीझ पैदा करता है. हमें हिन्दी के विकास प्रसार के लिए काम करना चाहिए लेकिन संयमित होकर न कि संयम खोकर, क्योंकि राजभाषा हिन्दी को सहेजना हमारा उत्तरदायित्व है. कोई भी देश अपनी राजभाषा के बिना तरक्की नहीं कर सकता क्यों कि अभिव्यक्ति का माध्यम तो भाषा ही होती है. इसी परिप्रेक्ष्य में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 सितम्बर, 1949 के दिन बहस में भाग लेते हुए तीन प्रमुख बातें कही थीं- किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता. कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती, भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में जो अपनी आत्मा को पहचाने, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिन्दी को अपनाना चाहिए. इसलिए ही 14 सितंबर को 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है. 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है.
भारत में हिन्दी को लेकर हमेशा से ही हंगामा होता रहा है. बड़े प्रयत्नों के बाद हिन्दी को राजभाषा का अधिकार मिला था. हालांकि भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति में बच्चों को प्राथमिक से ही अंग्रेज़ी पढ़ाने की बजाय रटाया जाता है. हिन्दी बोलने वालों के बीच अँग्रेजी कभी भी भाषा के रूप में नहीं देखी गई बल्कि एक स्किल के रूप में देखा जाता है. हमारे समाज़ में एक खामी है, बच्चा बिना अर्थ जाने किसी को भी अंग्रेज़ी में कविता रटकर सुना दे तो माता-पिता का मस्तक गर्व से ऊँचा हो जाता है. अब तो देश में हिन्दी की कविता केवल दो दिन '15 अगस्त' और '26 जनवरी' पर पढ़ी जाती है, इसके बाद में हिन्दी बोलने से सभी परहेज़ करते हैं. अंग्रेज़ी भाषी स्कूलों में तो किसी बच्चे द्वारा हिन्दी बोलने पर उसका वैचारिक बहिष्कार हो जाता है. बच्चे समझने की बजाय रटते रहते हैं, देखा जाए तो यह अवैज्ञानिक है. ऐसे अधिकांश बच्चे उच्च शिक्षा में माध्यम बदलते हैं तथा भाषिक कमज़ोरी के कारण खुद को समुचित तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते और पिछड़ जाते हैं. इस मानसिकता में शिक्षित बच्चा माध्यमिक और उच्च्तर माध्यमिक में मजबूरी में हिन्दी पढ़ता है, फिर विषयों का चुनाव कर लेने पर व्यावसायिक शिक्षा के दबाव में हिन्दी से दूर हो जाता है. अंग्रेजी में पारंगत होना अच्छी बात है, लेकिन हिन्दी भाषी होने के बावजूद भी हिन्दी न आना वाकई चिंता का विषय है.
आम लोग भाषा के जिस देशज रूप का प्रयोग करते हैं वह बात का आशय संप्रेषित करता है, किन्तु वह पूरी तरह शुद्ध नहीं होता. ज्ञान-विज्ञान में भाषा का उपयोग तभी संभव है, जब शब्द से एक सुनिश्चित हो. देखा जाए तो हिन्दी का प्रयोग न होने को दो कारण हो सकते हैं.. इच्छा शक्ति की कमी तथा भाषिक एवं शाब्दिक नियमों और अर्थ स्पष्ट न होना. हिन्दी के समाने सबसे बड़ी समस्या विश्व की अन्य भाषाओं के साहित्य को आत्मसात कर हिन्दी में अभिव्यक्त करने की तथा ज्ञान-विज्ञान की हर शाखा की विषयवस्तु को हिन्दी में अभिव्यक्त करने की है. अतः हिन्दी के शब्दकोष का पुनर्निर्माण बहुत आवश्यक हो गया है.. इसमें पारंपरिक शब्दों के साथ विविध बोलियों, भारतीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं, विविध विषयों और विज्ञान की शाखाओं के परिभाषिक शब्दों को जोड़ा जाना ज़रूरी है. जिससे आम जनमानस उसके साथ जुड़ा हुआ मसहूस करे. अंग्रेज़ी इसलिए ही ज़्यादा लोगों तक पहुंची है कि उसमें सुधार की गुंजाईश ज़्यादा होती है. नये शब्दकोशों में हिन्दी के हजारों शब्द समाहित किये गये हैं, किन्तु कई जगह उनके अर्थ, भावार्थ आदि गलत हैं. हिन्दी में अन्यत्र से शब्द ग्रहण करते समय शब्द का लिंग, वचन, क्रियारूप, अर्थ, भावार्थ तथा प्रयोग शब्द कोष में हो तो उपयोगिता में वृद्धि होगी. हिन्दी के हजारों भाषाविदों को हिन्दी प्रेमियों को मिलकर करना चाहिए. विध विषयों के अनुभवी लोग अपने विषयों के शब्द-अर्थ दें, जिन्हें हिन्दी शब्द कोष में जोड़ा जाये..
हिन्दी भाषाविदों को भी थोड़ा अपना स्वभाव बदलना होगा, थोड़ा उदार बनना होगा. बदलती हुई पीढ़ी को बिल्कुल लकीरों में चलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए. हिन्दी लिखने - बोलने पर थोड़ा मिश्रित भाषाओं के शब्दों की उपयोगिता को भी समझना होगा. अतः भाषाविदों के साथ ही हमारे समाज में हिन्दी के प्रति एक भाव होना चाहिए, केवल दो चार दिनों हिन्दी बोलने के नाटक करने की बजाय निरंतर हिन्दी बोलने का प्रयास होना चाहिए. पूरे साल हिन्दी का बहिष्कार करने के बाद दो चार दिनों उसका सम्मान करने के नाटक से बचना होगा... हमें भाषा को स्वीकार करने सहेजने की ओर बढ़ना चाहिए. हालांकि आज के दौर में आसान नहीं है, लेकिन अपनी राजभाषा हिन्दी को समृद्ध करने एवं बचाए रखने, निरंतर विकास के साथ आने वाली पीढ़ियों को जोड़ना चाहिए, जिससे भविष्य में हिन्दी और विकराल रूप धारण न धारण कर ले. हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कट्टर हो जाना है, बल्कि सभी भाषाओं की आवश्यकता एवं महत्व को कायम रखना है. तकनीकी विषयों के रचनाकारों को हिन्दी का प्रामाणिक शब्दकोष, व्याकरण की पुस्तकें अपने साथ रखकर जब जैसे समय मिले, पढ़ने की आदत डालनी होगी. हिन्दी की शुद्धता से आशय उर्दू, अंग्रेज़ी यानी किसी भाषा, बोली के शब्दों का बहिष्कार नहीं, अपितु भाषा के संस्कार, प्रवृत्ति, रवानगी, प्रवाह तथा अर्थवत्ता को बनाये रखना है. चूँकि इनके बिना कोई भाषा जीवंत नहीं होती.
दिलीप कुमार पाठक

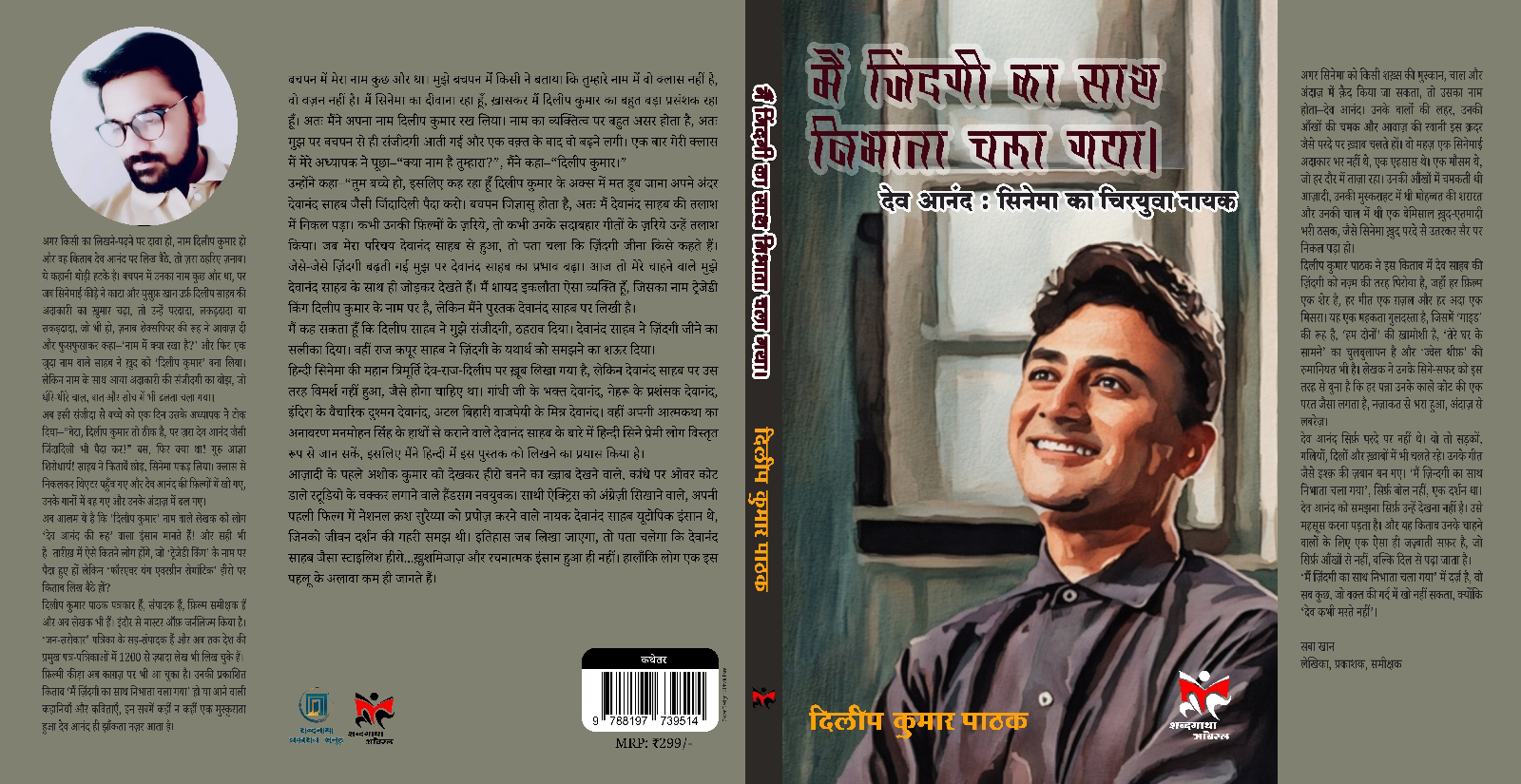


Comments
Post a Comment