*किसानों के प्रति सिनेमा की असंवेदनशीलता*
*किसानों के प्रति सिनेमा की असंवेदनशीलता*
----------------------------------------------------------
सिनेमा हमारे समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन जब बात किसानों एवं उनकी समस्याओं की आती है, तो यह आईना धुँधला पड़ जाता है. अब तक के सिनेमा इतिहास में किसानों को केंद्र में रखकर बनाई गई फ़िल्मों का जिक्र करें तो फ़िल्मों की अपेक्षा उँगलियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन फ़िल्में नहीं है.. यही कारण है कि भारतीय किसान उपेक्षित हैं. बीते कुछ सालों पहले कड़ी सर्दी में देश भर के किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया था. कड़ी सर्दी में किसानो ने डेरा जमाया हुआ था, किसानों का कहना था - "सरकार ने तीन कृषि कानून बनाए हैं, हमें वो स्वीकार नहीं हैं. दिल्ली में कड़ाके की सर्दी में किसानो ने हौसला नहीं छोड़ा, और जमे रहे. बुरे दौर से गुज़र रही मीडिया कहें या पथभृष्ट कहें इसी मीडिया ने किसानों की आवाज़ नहीं दिखाई, बल्कि किसानो को ही कठघरे में खड़ा कर दिया. हमारे देश में किसानों को अन्नदाता कहकर पुकारा जाता है, लेकिन अपने ही मुल्क में अन्नदाता को लाठियां, गोलियां, गालियाँ, साथ ही आतंकवादी जैसी गालियाँ भी खानी पड़ी. कुछ दिनों तक सरकार ने सुना ही नहीं जैसे किसानो का आंदोलन अस्तित्व में ही नहीं है. वैसे भी सरकारें सुनती कहाँ हैं!! किसानो ने सरकार की कोई भी बात नहीं मानी आख़िरकार सरकार को अपने नए तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े...ये आंदोलन देश में किसानों की स्थिति एवं हैसियत बयां करता है. इस आंदोलन में किसानो को किस दमन से गुजरना पड़ा उसको सोचकर एक संवेदनशील आदमी सिहर जाए. किसानो को दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया, उन्हें घुसने तक नहीं दिया गया. जबकि हमारे देश में सभी को अपनी आवाज़ उठाने का हक हासिल है, और यह हक हमारा संविधान देता है. किसानो को आतंकी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, किसानो का दमन किया गया, शोषण किया गया. एक आंकड़े के अनुसार इस आन्दोलन में 700 से ज़्यादा किसानो ने शहादत दी. आख़िरकार सरकार ने अपने कानून वापस ले लिए. हमारे देश के अन्नदाता की हालत बहुत ख़राब है, बहुतेरे लोग किसानो को इंसानो की श्रेणी में नहीं रखते... हमारे देश में जब अन्नदाता का भी दमन कर दिया जाता है तो उनकी इज्ज़त कौन ही करेगा?? हर विषय पर फ़िल्में बनाने वाला हिन्दी सिनेमा का अभी तक ऐसा कोई फ़िल्मकार सामने नहीं आया कि किसानों के आंदोलन, नृशंसता पूर्वक किए उस दमन को सिल्वर स्क्रीन पर उतार सके!! बहुत से संवेदनशील मुद्दो पर हिन्दी सिनेमा की बेरुखी खलती है.
हाल फिलहाल बेंगलुरु में हुई एक घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा ! जीटी वर्ल्ड मॉल में अपने बेटे के साथ आए किसान को अंदर नहीं घुसने दिया. अंदर न घुसने देने का कारण कि तुमने धोती - कुर्ता पहना हुआ है, लिहाज़ा आपको फिल्म देखना है तो अपना लिबास बदल कर आइए. सबसे बड़ी बिडम्बना यह है कि जिस देश की अधिकांश आबादी धोती - कुर्ता पहनती हो, जिस राज्य में यह घटना हुई, उस राज्य का परम्परागत पहनावा ही धोती है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं धोती पहनता हो उस राज्य के राजधानी में एक व्यक्ति को धोती पहनने पर इंसान ही नहीं समझा गया... जब किसानो को पहनावे के कारण फ़िल्में ही देखने की इजाजत नहीं दी जा रही, उस देश में किसानो पर फ़िल्मों का निर्माण होना बड़ा कठिन है. या यूं कहिए कि किसानों पर बनी फ़िल्मों का जोखिम कौन उठाए? वैसे भी किसान कौन सा थिएटर जाकर फ़िल्में देखते हैं. हालांकि बाद में प्रशासन से उस मॉल को स्थायी रूप से बंद करा दिया, लेकिन यह घटना देश की क्रूर सच्चाई को बयां करती है.
सूखा, बाढ़,गर्मी, या सर्दी हो कोई भी मौसम हो सबसे ज्यादा किसानो को ही भोगना पड़ता है. पूरी दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है, लेकिन एक सवाल किया जाना चाहिए क्या दौलत खाकर पेट भर सकता है? नहीं भर सकता, उसके लिए रोटी की आवश्यकता होती है. अब सवाल उठता है कि जब किसान सबसे क़ीमती रोटी के लिए अनाज उगाते हैं तो उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन किसानो की दुर्दशा भारत की हक़ीक़त है. एक सवाल उठता है अगर किसानो की स्थिति अच्छी होती तो वे अपने बच्चों को ज़मीन बेचकर पढ़ने के लिए शहर क्यों भेजते? जबकि ज़मीन तो किसान के लिए माँ की हैसियत रखती है, लेकिन जैसे किसान अपनी जीवन आभाव में काटता है तो वो नहीं चाहता कि उसका बेटा किसान बने. जबकि डॉ का चाहता है उसका बेटा डॉ बने, इंजीनियर चाहता है उसका बेटा इंजीनियर बने. क्योंकि आज भी किसानी को प्रोफेशन नहीं माना जाता.
हमारे मुल्क में प्रोफेशन उसे ही माना जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो या फ़िर वो जो ऑफिस जाता हो. आज भी कृषि को किसी पेशे की नजर से नहीं देखा जाता है, यही कारण है कि आने वाली पीढ़ियों का कृषि से मोह भंग होता जा रहा है.. वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, आदि ही प्रोफेशन माने जाते हैं जिन पर खूब फ़िल्में बनाई जाती हैं, समाज में हाशिए पर खड़े किसानो को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाने के लिए नज़र ही नहीं पड़ती. उन हीरोज़ के बारे में बहुत कम दिखाया जाता है जो दिन रात एक करके सबका पेट भरते हैं. सच्चाई यह भी है कि सिनेमा ने अभी तक न तो ढंग से किसानो पर फ़िल्में बनाई और न ही उनकी समस्याओं को इस लिहाज से दिखाया. हालाांकि कुछ फिल्मकारो ने किसानों पर फ़िल्में भी बनाई और किसानों की समस्याओं को बखूबी पर्दे पर उतारा.. जिनमे विमल रॉय, महबूब खान, दिलीप कुमार, बी आर चोपड़ा, मनोज कुमार आदि इसके लिए ये सब आदर के पात्र हैं.
सिनेमा में किसानों से संबधित फ़िल्मों की बात की जाए तो, इतने बड़े फिल्मी इतिहास में किसानों पर या उनकी समस्याओं पर बनी फ़िल्मों को उँगलियों में गिना जा सकता है. कितनी हैरत की बात है, जिस देश में सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता हो, जिस देश की जनता 70 %, किसानी पर आश्रित हो, वहीँ किसी भी पीढ़ी से पूछिए उसकी पिछली या खुद की पीढ़ी का सीधा ताल्लुक खेत - खलिहान से ही मिलेगा. फ़िर भी किसानों की खस्ताहाल ज़िन्दगी फ़िल्मकारों को दिखती नहीं है. आज देश के शहरो में बढ़ती हुई आबादी के पीछे किसानो में गांवों में बढ़ता असंतोष या भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना उन्हें गांवो से शहरो की ओर खींच ला रही है. फ़िर भी हमारे सिनेमा के लोगों को समाज की विकृतियाँ नहीं दिख रहीं ! फिल्म निर्देशक किसान विमर्श पर फ़िल्में बनाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते. अब देखा जाए तो हिन्दुस्तानी सिनेमा की सबसे पहली कल्ट फ़िल्म किसान की परेशानियों पर ही बनाई गई महान फ़िल्मकार विमल रॉय ने 'दो बीघा ज़मीन' बनाकर हिन्दुस्तानी सिनेमा को बताया कि कल्ट फिल्म कैसे बनाते हैं.
'दो बीघा ज़मीन' पहली ऐसी फिल्म थी, जिसे बेशुमार वैश्विक ख्याति मिली. होना तो यह चाहिए था कि इस फिल्म के बात देश में किसानों पर बहुत सारी फ़िल्म का निर्माण होता लेकिन इस सब्जेक्ट पर फ़िल्मकारों ने कोई ख़ास रुचि नहीं ली. हालाँकि कुछ फिल्मकारों ने किसानों की व्यथा पर फ़िल्में बनाई जो दुनिया की महानतम फ़िल्मों में शुमार हुई. फ़िर कभी - कभार इक्का - दुक्का किसानो पर फ़िल्में बनी जैसे 'मदर इन्डिया' , 'लगान' , 'पीपली लाइव' , 'गंगा जमुना' , 'मंथन', 'गाभ्रीचा पाऊस' , 'उपकार' , 'कड़वी हवा' , जैसी बहुत कम फ़िल्में बनाई गई हैं. 'मदर इन्डिया' एवं 'लगान' को तो ऑस्कर में भी जगह मिली...
भारतीय सिनेमा में उन फ़िल्मों का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है जिन्होंने किसानों जैसे संवेदनशील मुद्दो पर फ़िल्म बनाकर खुद की सिनेमाई यात्रा सार्थक की. किसी भी संवेदनशील मुद्दो पर पुराने मकड़जालों को साफ़ करने का श्रेय सबसे ज़्यादा महान फ़िल्मकार 'विमल रॉय' को ही जाता है. जब तक 'दो बीघा ज़मीन' का जिक्र विस्तृत नहीं होगा किसान विमर्श पूरा नहीं हो सकता.
*किसानों की ज़िन्दगी पर बनी फ़िल्मों का जिक्र*
--
*किसानों की ज़िन्दगी पर बनी पहली फिल्म "दो बीघा ज़मीन*
--------------------------------------------------------------------------
दो बीघा ज़मीन अपने नाम से ही अपना परिचय दे रही है कि इसका सब्जेक्ट क्या है. यह फिल्म 'रवींद्रनाथ टैगोर' द्वारा लिखित बंगाली उपन्यास 'दुई बीघा जोमी' पर आधारित है. यह फिल्म गरीब किसानों पर साहूकारों के अन्याय की कहानी कहती है. फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है भयंकर अकाल पड़ जाने के बाद जब गांव में बारिश होती है तो गांव का छोटा किसान शंभू अपने परिवार सहित खुश है कि मुद्दतों बाद बारिश हुई है. यह सच है एक अदद बारिश की ज़रूरत एक किसान से ज्यादा कौन समझ सकता है. शम्भू गांव के रईस से 65 रुपए उधार ले लेता है, लेकिन देनदार की सबसे ज़्यादा नज़र शंभू की ज़मीन पर हैै. वो शहर के सेठों के साथ मिलकर गांव में कारख़ाना लगाना चाहता है. शंभू बेचारा इस कुटिल चाल को समझ नहीं पाता. एक गरीब किसान परिवार जो अपनी ज़मीन को माँ मानता है, कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे बहुमूल्य चीज क्यों देगा? आखिरकार शंभू सोच लेता है कि मैं कमाकर इसके 65 रुपए चुका दूँगा... कम पढ़ा लिखा शंभू बेचारा पेट काटकर पैसे इक्कठे करने लगता है. एक दिन बड़ा खुश होकर पैसे सेठ के पास लौटाने जाता है, तब ही शंभु को पता चलता है कि जो कर्ज़ लिया था वो 65 नहीं बल्कि 253 रुपए हैं. बेचारा एक गरीब किसान अपने हक़ की लड़ाई के लिए अदालत जाता है लेकिन हमारे देश में कानून हमेशा से ही गरीबो के लिए और अमीरों के लिए और रहा है. उम्मीद के मुताबिक शंभू केस हार जाता है, उसे तीन महीने के अंदर क़र्ज़ चुकाने का हुक्म मिलता है वरना उसकी ज़मीन नीलाम हो जाएगी...
पूँजीवादी लोग कैसे गरीबो पर ज़ुल्म करते हैं, कैसे 65 के 253 हो जाते हैं. यह एक फिल्म की सच्चाई नहीं है, बल्कि किसानो के शोषण की कहानी बयां करती है. बेचारा एक ग़रीब निर्णय लेता है कि मैं अपनी ज़मीन लेकर रहूँगा. तब कैसे एक गरीब आदमी अपने माता - पिता पत्नी बच्चों को छोड़कर पैसे कमाने के लिए विशाल शहर कोलकाता चल पड़ता है. वो उस उम्मीद से ही निकलता है कि पैसे कमाकर लाएगा और अपनी ज़मीन छुड़ा लेगा... कोलकाता जैसा विशाल शहर कम पढ़े लिखे शम्भू की खासी कठिन परीक्षा लेता है, एक गांव का आदमी कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा खींचता है. बाद में अपने पिता के पीछे वो बच्चा कोलकाता पहुंच जाता है. भूखा बच्चा चोरी कर लेता है, तब बाप शम्भू रोते हुए अपने बेटे से कहता है किसान का बेटा होकर तू चोरी करता है! इस सीन को देखकर किसी भी संवेदनशील इन्सान का कलेजा हाथ में आ सकता है. पेट - पीठ के बीच का फर्क़ खत्म कर देने वाली भूख एक बच्चे को पेट भरने के लिए चोरी की इजाज़त नहीं दे सकती , ये किसानो के सिद्धांत रहे हैं. गौरतलब किसानो को बदले में क्या मिला? शोषण अपमान! दो बीघा ज़मीन महज एक फिल्म नहीं है बल्कि समूचे हिन्दुस्तान के किसानो की वेदना थी. जिसे बड़ी ही सहजता के साथ महान फ़िल्मकार 'विमल रॉय' ने पर्दे पर पेश किया. इस फिल्म को हिन्दुस्तान की पहली कल्ट फिल्म का मुकाम हासिल है. विमल रॉय ने इस फिल्म को बड़ी सहजता से इसलिए भी दिखा पाए क्योंकि उन्होंने खुद के जीवन में पलायन की त्रासदी सही है.
'निरुपा रॉय' , महानतम ऐक्टर 'बलराज साहनी' दोनों की अदाकारी लोगों के दिनों में आज भी रची बसी हुई है. बड़े अफ़सोस के साथ इस बात को स्वीकार करना होगा कि दो बीघा ज़मीन जैसी बड़ी सफलता के बाद भी हिन्दी सिनेमा ने इस टॉपिक से दूरी बना ली. जब - जब हिन्दुस्तान में किसानो पर किसी भी तरह की ज्यादती होगी, तो दो बीघा ज़मीन अपने निर्माण की उपयोगिता सिद्ध करती रहेगी.
*कृषि एवं सामाजिक सुधार पर श्याम बेनेगल का सिनेमाई मन्थन*
-----------------------------------------------------------------------
'श्याम बेनेगल' समानांतर सिनेमा के अग्रणी शिल्पकार माने जाते हैं. बेनेगल की अथक मेहनत एवं सरोकार को सिनेमा के धरातल पर उतारने में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है. हिन्दी सिनेमा जब 'राजेश खन्ना' के सुपरस्टार वाले सुपरस्टारडम एवं 'अमिताभ बच्चन' की आँधी के पीछे अपना सामान ले कर पीछे - पीछे चल रहा था, तब 'श्याम बेनेगल' मन्थन जैसी किसानों की दशा पर फ़िल्मों का निर्माण कर रहे थे. दरअसल कृषि फ़िल्मों का निर्माण अपने आप में एक जोखिम का काम रहा है, क्योंकि मेहनत, शोध के साथ धरातल पर काम करना पड़ता है. जबकि एक बड़ा वर्ग ऐसी फ़िल्मों को बोरिंग कहकर खारिज कर देता है.
गांव के किसानों पर आधारित मंथन एक ऐसी फिल्म है, जो हिन्दी सिनेमा में अपने प्रयोगों के लिए याद की जाएगी. 'मन्थन' फ़िल्म को सामूहिक 5 लाख किसानों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था ! जी हाँ यह पढ़कर पाठकों को आश्चर्य हो सकता है, कि यह क्या बात है. दरअसल यह किसानों के फण्ड पर बनाई जाने वाली फिल्म है. किसानो ने किसी तरह दो-दो रुपये बचाकर फिल्म में लगाए थे. इस फिल्म को व्यापारिक एवं समीक्षात्मक खूब सराहना मिली. फ़िल्म की सफलता में दो नैशनल अवॉर्ड ने चार चांद लगा दिए थे. इस नायाब फ़िल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी भेजा गया था. फ़िल्म ‘मंथन’, श्वेत क्रांति एवं किसानों पर आधारित थी. 1976 में आई इस फिल्म को 'श्याम बेनेगल' ने निर्देशित किया था. श्वेत क्रांति का मतलब दुग्ध क्रांति से है.
जिस संदर्भ में फ़िल्म का निर्माण किया गया था. फिल्म के निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा पर फ़िल्मकार काम करता है. आमतौर पर जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो उसके लिए स्टार्स की कास्टिंग के साथ-साथ बजट का भी प्लान किया जाता है. उस बजट के हिसाब से ही निर्माता तय करता है, कि फिल्म कैसे बनेगी किस दिशा में जाएगी. चूँकि प्रत्यक्ष रूप से इस फ़िल्म में कोई प्रोड्यूसर नहीं था, अंततः इसके आधिकारिक तौर पर प्रोड्यूसर श्याम बेनेगल ही थे. ‘मंथन’ फिल्म का निर्माण समय की मांग एवं तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया था. किसानों से चंदा इकट्ठा करके फिल्म के लिए फंड इकट्टा किया गया था. मंथन 70 के दशक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है और हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म है, जिसे चंदा इकट्ठा करके बनाया गया था. इस फ़िल्म को कल्ट फ़िल्मों की फेहरिस्त में शामिल किया जाए तो शायद सही होगा.
1976 में इमर्जेंसी के दौरान रिलीज हुई ‘मंथन’ में किसानों और पशुपालकों के संघर्ष को बड़े ही मार्मिक अंदाज में फिल्मी पर्दे पर उतारा गया था. इस फिल्म में सामजिक असंतुलन के एक - एक रेशे को खोला जाता है. ‘मंथन’ की कहानी 'वर्गीज कुरियन' और श्याम बेनेगल दोनों ने लिखी थी. 'वर्गीज कुरियन' को भारत में वाइट रेवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति का ध्वजवाहक कहा जाता है. उन्होंने ही दूध के प्रोडक्शन में भारत को दुनिया में नंबर वन बना दिया था. 'वर्गीज कुरियन' को मिल्क मैन भी कहा जाता है. वर्गीज कुरियन ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी. जिसके कारण भारत में श्वेत क्रान्ति आ गयी थी. भुखमरी, बेरोज़गारी चरम पर थी, तब भारत पूरी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में कोई मुकाम नहीं रखता था, चूंकि कृषि के लिहाज से भारत अग्रणी रहा है. 'वर्गीज कुरियन' जैसे समाज़ सुधारक लोगों का अग्रणी साथ मिला तो दूध के उत्पादन में पूरी दुनिया में शीर्ष पर पहुंच गया था. 'श्याम बेनेगल' और वर्गीज कुरियन ने मिलकर इस एतिहासिक सफलता को फिल्म के रूप में उतारने का फैसला किया. फिर ‘मंथन’ बनने का सिलसिला शुरू हुआ.
चूंकि ‘मंथन’ किसानो पर आधारित फिल्म थी, जिसका उद्देश्य मात्र किसानों को कवर करना था. श्याम बेनेगल की फ़िल्मों में अदाकारी के लिहाज से देखना एवं उस सरोकार को अपने अंदाज़ में देखना हमेशा से सर्वोत्तम रहा है. यूं लगता है श्याम बेनेगल जैसे फ़िल्मकारों ने समाज के उस दंश को सहा होगा तब ही उसको सिल्वर स्क्रीन पर उतार पाए. फिल्म की स्टारकास्ट में 'गिरीश कर्नाड' , 'कुलभूषण खरबंदा' , 'स्मिता पाटिल' , 'नसीरुद्दीन शाह' , 'अमरीश पुरी' , 'अनंत नाग' और 'मोहन अगाशे' जैसे मंझे हुए अदाकारों की फ़ौज 'श्याम बेनेगल' ने खड़ी कर दी. चूंकि फिल्म की कहानी उन किसानों पर आधारित थी, जो गांवों में सहकारी समिति बनाने में लगे थे. ऐसे में कोई भी फ़िल्म निर्माता इस फिल्म पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था. फिल्म का बजट 10 से 12 लाख रुपये था. पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा था. ऐसे में किसान सरोकार की फिल्म ‘मंथन’ बनाने का सपना कैसे पूरा हो? तब 'वर्गीज कुरियन' और 'श्याम बेनेगल' ने एक तरीका निकाला. उन्होंने किसानों से 2-2 रुपयों का चंदा इकट्ठा करने का फैसला किया. 'वर्गीज कुरियन' को लोग मानते थे एवं उनकी नीतियों से परिचित थे. उन्होंने गुजरात में जो सहकारी समिति बनाई थी. उससे करीब 5 लाख किसान जुड़ चुके थे. कुरियन उस वक्त अमूल को-ऑपरेटिव के संस्थापक थे. उन्होंने किसानों से अपील की वो दूध बेचकर जो कमाते हैं, उससे 2-2 रुपये दान कर दें ताकि जो चंदा इकट्ठा हो, उसकी मदद से फिल्म बनाई जा सके और किसानों के संघर्ष एवं दर्द को पूरी दुनिया को दिखाया जा सके. जिससे लोगों को पता चले कि जो शहरों में लोगों को दूध मिलता है, वो इतनी आसानी से नहीं पैदा होता उसके लिए किसी ने अपनी ज़िन्दगी गोबर, चारे में बिता दीं, बदले में उनके बच्चों को शिक्षा तो दूर की कौड़ी दो वक़्त की रोटी भी मुश्क़िल से नसीब होती है. किसानों ने बात मान ली. उस वक्त कुरियन की गुजरात में बनाई सहकारी समिति से करीब 5 लाख किसान जुड़े थे. उन सभी किसानों ने अपनी कमाई से 2-2 रुपये बचाए और फिल्म ‘मंथन’ में लगा दिए. इस तरह ‘मंथन’ एक ऐसी फिल्म बन गई, जिसे 5 लाख किसानों ने फिल्म को फाइनेंस किया. 'श्याम बेनेगल' जैसे कला फ़िल्मों के पुरोधा हमेशा ही ऐसा सिनेमा गढ़ते रहे, जिससे लोगों में चेतना का प्रसार हो.
‘मंथन’ फिल्म तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद रिलीज हुई, रिलीज होते ही फिल्म हिट हुई एवं लोगों के मानस पटल पर अंकित हो गई. इसे बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट स्क्रीप्ले के लिए 2 नैशनल अवॉर्ड मिले. ‘मंथन’ फिल्म को 1976 भारत की तरफ से ऑस्कर में भी भेजा गया. ‘मंथन’ की शूटिंग भी गुजरात के सान्गवा गांव में हुई थी. इस गांव में फिल्म के कलाकारों ने करीब 45 दिनों तक डेरा डाला था. एवं गांव को उस ज़िन्दगी को बड़े नजदीक से देखा था. तब कहीं.... फिल्म की कहानी के किरदारों को पर्दे पर उतार सके. फिल्म में गांव के रहने वाले किसानों में भी काम किया. श्याम बेनेगल उन किसानों को रोजाना 7 रुपये दिया करते थे, जो फार्म में पूरे दिन काम करने के बाद सिर्फ 5 रुपये ही कमा पाते थे.
फिल्म ‘मंथन’ लोगों के सामूहिक प्रयास को दर्शाती है. गुजरात के खेड़ा जिले के ‘दुग्ध क्रांति’ किसानो की सहकारिता का एक सशक्त उदाहरण है. इसी से प्रेरित यह फिल्म किसानों के पैसे से ही बनाई गई है. जिसमें उनके संघर्षों का ही प्रतिफल है. फिल्म में दूध बेचने वाले किसानों की सहकारी समिति (सोसाइटी) बनाने और उसमे आने वाली कठनाईयों को फ़िल्माया गया है. एक युवा वेडनरी डॉक्टर राव (गिरीश कर्नाड) जो मानवतावादी और समाजवादी मूल्यों को मानने वाले हैं. गांव में सोसाइटी बनाने का प्रयास करता है. लोगों को जागरूक करता है. गांव के लोग लंबे समय से एक नेता, व्यापारी 'अमरीश पुरी' की ‘डेयरी में दूध बेचते रहे होते हैं. मगर वह उचित कीमत से बहुत कम कीमत देता रहा है. चूंकि, वह साहूकार भी है इसलिए किसान उस पर कई तरह से आश्रित हैं. संकट पैदा करके ‘सहायता’ की कूटनीति पर भी चलता है. इन सब कारणों से किसानों का उसके चंगुल से निकलना आसान नहीं था. इस फिल्म में भोला (नसीरुद्दीन शाह) जैसे लोग जो हक़ीक़त समझते हैं वो भी सशक्त रोल में हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी रूप में डॉ राव (गिरीश कर्नाड) की आवश्यकता होती है. फिल्म में एक कम पढ़ी लिखी विंदु (स्मिता पाटिल) जैसी साहसी महिला भी है लेकिन एक आदमी की कमी के कारण वो भी शोषित है. फिल्म में गिरीश कर्नाड सबसे सशक्त रोल में हैं, जो फिल्म में लीड ऐक्टर के तौर पर हैं. चुस्त-दुरुस्त कहानी के साथ बेह्तरीन कथानक फिल्म को कालजयी साबित करता है.
फिल्म का क्लाईमैक्स बेहद उम्दा होता है. आज सबकुछ ज़रूरी नागरिक संसाधनो को निजी हाथों में बेचे जाने के इस क्रूर, पूंजीवाद के दौर में सहकारिता की अवधारणा अब ज़मीन पर दिखाई नहीं देती. मगर मानवीय मूल्यों एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा सहित आम ज़न मानस आत्मसम्मान का सामजिक समानता का यही मूल रास्ता है. आज के पूंजीवाद मानसिक ग़ुलामी के दौर में इसके लिए व्यक्ति को भी अपने स्वार्थ से ऊपर व्यापक समाज के हित के बारे में सोचना होगा. अन्यथा सामाजिक द्वेष के साथ असमानता के साथ दुनिया तो चल ही रही है. आगे भी चलती रहेगी, लिहाज़ा लोगों में खुद के अधिकारों के प्रति चेतना तो हो. श्याम बेनेगल हमेश से ही ऐसी ज़नमानस की फ़िल्मों का निर्माण करते रहें हैं. ऐसी फ़िल्मों का निर्माण एक अर्थिक रूप से नुकसानदेह होता है, चूंकि एक सृजनकर्ता का काम होता है कि समाज तो उसे बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन वो इस समाज को दे रहा है? समाज के निर्माण में सबसे ज्यादा जवाबदेही रचनाकारों, साहित्यकारों की होती है. श्याम बेनेगल जैसे समानान्तर सिनेमा के यादगार सृजनकर्ता हमेशा अपनी बेह्तरीन 'मन्थन' जैसी फ़िल्मों के कारण अमर रहेंगे.....
*नया दौर*
---------------
औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में 'बी. आर. चोपड़ा' ने फिल्म 'नया दौर' में किसानों की ज़िन्दगी एवं उनका दर्द दिखाया है. फिल्म नाम से ही सिद्ध होता है कि फ़िल्म का उद्देश्य क्या है. इसमें मजदूरों - किसानों का साझा संघर्ष दिखाया गया है. 'नया दौर' को कल्ट फिल्म का दर्जा प्राप्त है. फ़िल्म किसानों की जीविका के ऊपर आधारित है, कि कैसे ग़रीब अपने पेट के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं, लेकिन पूंजीपति इन मुश्क़िल परिस्थितियों में भी सुकून से पेट भी नहीं भरने देते. फ़िल्म ‘नया दौर’ में मशीन और मजदूर - किसान के बीच की लड़ाई एवं पेट की जंग दिखाई गई है. इस जंग में कैसे किसान विजयी होते हैं. 'दिलीप कुमार' की अदाकारी मन मोह लेती है.
इस सामाजिक संवेदनशील मुद्दे पर बनी फ़िल्म में 'दिलीप कुमार' एक ऐसे तांगे वाले की भूमिका में हैं, जो एक पूंजीपति को चुनौती देते हैं.. फिल्म में जल्दी पैसे कमाने के लिए सेठ बस सेवा की शुरुआत करता है, जिससे वहां के किसानों और मजदूरों की जीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है. यह पैसे वाला सेठ तांगों की जगह सड़कों पर बसों की स्वीकार्यता बढ़ाने के प्रयास में ग़रीब तांगे वालों के हितों की अनदेखी करता है.
किसानों और मजदूरों की समस्या को यह फिल्म अच्छे से दिखाती है. गरीबों की ज़िन्दगी के छोटे - छोटे मगर बहुत बड़े संघर्ष को सिल्वर स्क्रीन पर 'दिलीप कुमार' 'वैजयंतीमाला' , 'अजीत' आदि ने इतने बेहतरीन ढंग से दिखाया है कि देखने वाले भावुक हो जाते हैं. कैसे 'दिलीप कुमार' तांगे में बैठकर बस से रेस लगा लेते हैं इसमे आप तर्क ढूढ़ने निकलेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस संवेदनशील विषय पर निर्देशक, कलाकारों की मेहनत एवं उनकी मंशा पर सवाल नहीं किया जा सकता. कृषि, मेहनतकश लोगों के दर्द को बड़ी संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर दिखाने के लिए 'बी. आर. चोपड़ा' आदर एवं बधाई के पात्र हैं. आज जब किसानो की दुर्दशा का दौर चल रहा है, तब 'बी. आर. चोपड़ा' जैसे निर्देशकों की कमी शिद्दत से खलती है.
*गंगा - जमुना*
-------------------
डूबकर ऐक्टिंग करने वाले मेथड ऐक्टर 'दिलीप कुमार' फ़िल्म बनाने से खुद को दूर ही रखते थे. किसानो की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म 'मदर इन्डिया' 'दिलीप कुमार' को बहुत पसंद आई थी. पहले 'दिलीप कुमार' इस फिल्म में काम करने वाले थे लेकिन उन्होंने फ़िल्म में नर्गिस जी का बेटा बनने से इंकार करते हुए फ़िल्म छोड़ दिया. दिलीप साहब महबूब खान की 'मदर इन्डिया' छोड़ने की कसक पूरी करना चाहते थे. 'मदर इन्डिया' से प्रेरित होकर दिलीप साहब ने एक फिल्म 'गंगा - जमुना' पूर्वी उत्तरप्रदेश के ग्रामीण पृष्ठभूमि किसानों पर फिल्म बनाने का सोचा. दिलीप साहब ने फिल्म भी उसी शिद्दत से बनाई जिस शिद्दत से अभिनय करते थे. लेकिन इस कालजयी फिल्म को बनाने में ऐसी मुश्किलें आईं कि दिलीप साहब ने फ़िल्म निर्देशन से हमेशा के लिए तौबा कर लिया. इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने दिलीप साहब की दलील खारिज करते हुए 250 से ज़्यादा कट लगाए. दिलीप साहब की फिल्म में 'पंडित नेहरू जी' के दखल के बाद सेंसर ने रिलीज होने की अनुमति प्रदान की... इस लिहाज से दिलीप साहब को फ़िल्म बनाना काफ़ी महंगा पड़ा. हालाँकि दिलीप साहब ने एक ही फिल्म बनाई, लेकिन मुद्दा चुना तो किसानों का संवेदनशील मुद्दा.. तब के फिल्मकारों की किसानों एवं ज़न सरोकार पर प्रतिबद्धता दिखती है. पूर्वी उत्तरप्रदेश की पृष्ठभूमि पर बन रही फ़िल्म के लिए दिलीप साहब ने उस क्षेत्र का पूरी फिल्म यूनिट सहित दौरा किया था, और स्थानीय भाषा भी सीखा और किसानों के साथ समय भी बिताया तब कहीं किसानों की ज़िन्दगी पर फिल्म बना सके.. गौरतलब 'दिलीप कुमार' , 'वैजयंती माला' दोनों यूपी से ताल्लुक नहीं रखते थे.
1960 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म 'मुगल ए आज़म' में जब दिलीप साहब को साहिबे आलम के किरदार में सिने प्रेमियों ने बड़े - बड़े डायलॉग बोलते हुए उस भव्यता को देखा तो सिने प्रेमी उस भव्यता में खो गए थे.... और एक साल बाद 1961 में गंवाई किरदार 'गंगा जमुना' में देखा तो लोगों को लगा 'अरे दिलीप कुमार तो अपने ही जैसे हैं'...ये होते हैं हीरो जो समाज के साथ चलते हुए समाज की समस्याओं पर फ़िल्मों का निर्माण करते हैं. आज भी ज़न सरोकार की फ़िल्में बन रही हैं लेकिन जब किसानों के मुद्दे पर फ़िल्में गिनी जाएं तो उँगलियों की अपेक्षा फ़िल्में कम पड़ जाती हैं.
*मदर इन्डिया*
--------------------
महान फ़िल्मकार 'महबूब खान' की फ़िल्म 'मदर इन्डिया' से भला कौन परिचित नहीं होगा. ये किसान परिवार के संघर्ष एवं उसकी चुनौतियों को पर्दे पर पेश करती हुई फ़िल्म है. गौरतलब है कि 'महबूब खान' इसी फिल्म को पहले 'औरत' नाम से बना चुके थे, बाद में उन्होंने पूरी की पूरी स्टारकास्ट बदल डाला , सिवाय लाला के.. नारी सशक्तिकरण के लिए इस फिल्म का उदहारण दिया जाता है, लेकिन ये फ़िल्म एक माँ या यूं कहें कि किसान माँ की चुनौतियां सिल्वर स्क्रीन पर दिखाती है.. एक महिला अपने बच्चों को किन परिस्थितियों में पालती है, और अपने स्त्रीत्व मूल्यों को बचाए रखती है. ये फिल्म अपने आप में मुकम्मल दस्तावेज है. फ़िल्मकार 'महबूब खान' इस फिल्म के लिए शिद्दत से याद किए जाते हैं. 'नर्गिस' ने भारतीय महिलाओं की ज़िन्दगी को जिस शिद्दत से पर्दे पर दिखाया बाद में वो तस्वीर हिन्दुस्तान के सिनेमा की तस्वीर बन गई. 'राजेन्द्र कुमार' , 'सुनील दत्त' दोनों इस फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर छा गए थे, जिनकी आभा आज भी दिखाई देती है. ये सच है कि 'मदर इन्डिया' केवल एक बार बनाई जाती है, लेकिन हमारे फिल्मकारों का इंट्रेस्ट ऐसी फ़िल्मों के निर्माण पर ज़रा कम ही दिखता है, जो काफ़ी अफ़सोसनाक है.
*उपकार*
-----------------
'जय जवान जय किसान' का नारा देने वाले क्रान्तिकारी एवं पूर्व प्रधानमंत्री 'लाल बहादुर शास्त्री' देश के महानतम नेताओं में याद किए जाते हैं. सन 1965 में उन्होंने देश को 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया था. यह वो समय था जब देश पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था. भारत ने यह युद्ध जीत लिया था. इसी साल 'लाल बहादुर शास्त्री' ने दिग्गज एक्टर और फिल्ममेकर' मनोज कुमार' को एक फिल्म बनाने की सलाह दी थी. दरअसल, साल 1965 में मनोज कुमार की फिल्म 'शहीद' की स्क्रीनिंग दिल्ली में हुई थी. इसी स्क्रीनिंग में लाल बहादुर शास्त्री भी शामिल हुए, इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई. तब' लाल बहादुर शास्त्री' ने मनोज कुमार से कहा कि आप सेना और सुरक्षा पर फिल्में बनाते हैं. लेकिन जवानों के साथ देश का भरण-पोषण करने वाले किसानों पर कोई फिल्म नहीं बनाते. शास्त्री जी की बात से 'मनोज कुमार' काफी प्रभावित हुए...
'मनोज कुमार' ने 'लाल बहादुर शास्त्री' की सलाह को स्वीकार कर ट्रेन से मुंबई लौट गए और ट्रेन के सफर में मात्र 24 घंटे में ही पूरी कहानी लिख डाली थी. जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का प्रभाव आजकर भारतीय सिने प्रेमियों में दिखता है, यह फिल्म 'लाल बहादुर शास्त्री' के दिए नारे 'जय जवान, जय किसान' पर आधारित थी, जिसमें सेना और किसान दोनों को देश का सबसे बड़ा कर्ता-धर्ता और रक्षक बताया था. 'उपकार' ने देश-दुनिया में बहुत जबरदस्त कलेक्शन किया था. फिल्म का गाना 'मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती' जैसे गाने हिट हुए कि आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर स्कूल-कॉलेजों से लेकर घरों तक खूब बजाए और सुने जाते हैं. ऐसी जवानों एवं किसानों पर ज़नसरोकार की फ़िल्मों का निर्माण करने के लिए उन्हें 'भारत कुमार' कहकर पुकारा जाने लगा.
*पीपली लाइव*
---------------------
जब जब व्यापारिक अदाकारों के सार्थक सिनेमा में योगदान की बात आएगी, 'आमिर खान' को इज्ज़त की निगाह से देखा जाएगा. 'पीपली लाइव' दरअसल यह फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई है. पीपली एक गांव है जहां गरीब किसानो द्वारा लोन न चुकाए जाने के कारण सरकार उनकी जमीन छीन रही है, जिससे कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली है. वहीँ यह कैसी बिडम्बना है कि वही सरकार मदद करने का आडंबर भी कर रही हैं. अतः वहां एक किसान नत्था का भाई चाहता है कि नत्था भी आत्महत्या कर ले ताकि उनके परिवार को मुआवजा मिल जाए, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं है. कुछ किसान और सोचते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं जिससे परिवार को मुआवजा मिल जाएगा . कुछ ही दिनों में चुनाव है अब उस गांव सहित नत्था चर्चा का विषय हो जाता है कि नत्था आत्महत्या करेगा या नहीं!!! मीडिया भी खूब तमाशा बनाता है लेकिन गरीबो की उस त्रासद स्थिति का किसी को कोई अंदाजा नहीं है. किसानो के इस संवेदनशील मुद्दे को उठाती फिल्म बहुत सारे प्रश्न छोड़ जाती है जो स्तब्ध कर देते हैं.
*नीरोज़ गेस्ट्स*
---------------------
'नीरोज़ गेस्ट्स' एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका निर्देशन 'दीपा भाटिया' ने किया है और इसमें पत्रकार पी. साईनाथ ने काम किया है, जो पीपुल्स आर्काइव्स ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक हैं. नीरोज़ गेस्ट्स... एक डाक्यूमेंट्री है जो किसानो के एक संवेदनशील मुद्दे पर बनाई गई है. बहुतेरे लोगों को एक बेसिक बात समझ नहीं आती कि भला आत्महत्या से कोई हल निकलता है? ये किसान आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? ये एक छोटी सी मगर बड़ी बात है जो हर किसी को समझ नहीं आएगी कि किसान खुद को क्यों खत्म कर लेते हैं.
ये डॉक्यूमेंट्री इसी संवेदनशील मुद्दे को बेहतरीन तरीके से उठाती है. ऐसी डाक्यूमेंट्री और भी बनाए जाने की दरकार है. भले ही ऐसी डाक्यूमेंट्री की ज़्यादा चर्चा नहीं होती लेकिन ऐसे कन्टेन्ट की इस समाज को बहुत ज़रूरत है.
*कड़वी हवा*
---------------
जब भी ज़न सरोकार के सिनेमा की बात आती है तब 'संजय मिश्रा' इस व्यपारिक दौर में भी सबसे अव्वल दर्जे पर खड़े मिलते हैं. एक दौर में 'ओम पुरी' , 'नसीरूद्दीन शाह' , 'श्याम बेनेगल' जैसे कला फ़िल्मों के उस्तादों ने जो ज़मीन तैयार की थी, उस पर 'संजय मिश्रा' जैसे अदाकार एक उम्मीद जैसे लगते हैं. 'संजय मिश्रा' की प्रत्येक फिल्म झकझोर देने वाली होती है, लेकिन एक बुजुर्ग किसान की भूमिका में 'संजय मिश्रा' को देखने के लिए हिम्मत चाहिए क्योंकि किसी भी अति संवेदनशील इन्सान के लिए वो देख पाना आसान नहीं है.
निर्देशक 'नील माधव पांडा' की फिल्म 'कड़वी हवा' हमें उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है जिससे देश के किसान जूझ रहे हैं. फिल्म की कहानी सूखे की मार झेल रहे बुन्देलखण्ड एरिया की है. जहां के किसान सूखा पड़ने की वजह अपने खेत खो चुके हैं और बैंक का लोन ना चुका पाने के डर से आत्महत्या कर रहे हैं. देखा जाए तो केवल बुन्देलखण्ड नहीं बल्कि देश के किसानों की कमोवेश यही स्थिति है. फिल्म में यही डर एक अंधे बूढ़े बाप को भी सता रहा है कि कहीं उसका बेटा भी कर्ज ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या ना कर ले. कमाल के ऐक्टर 'संजय मिश्रा' फिल्म में एक अंधे बुजुर्ग किसान की भूमिका में हैं, जो अपने बेटे मुकुंद का कर्ज किसी भी तरह चुकाना चाहते हैं. वो बुज़ुर्ग किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा भी गांव के और किसानों की तरह आत्महत्या कर ले.
अतः वो कर्ज की रकम जानने के लिए बैंक पहुंच जाता है, लेकिन बैंक का वसूली अधिकारी उसे बैंक से डांट कर भगा देता है. कितनी विसंगतियों वाला हमारा सिस्टम है, दर-असल हमारे बैंकों में लिखा होता है "हमारे ग्राहक भगवान हैं, आपकी सेवा हमारा कर्तव्य है". लेकिन हमारे देश के बैंकों में गरीबो को बेइज्जत होना पड़ता है क्योंकि उनका लिबास रईसों की तरह नहीं होता.. किसानों पर फ़िल्में बनाने की दरकार यूँ भी इसलिए है कि देश के लोगों को पता चल पाए कि देश के किसानों की कितनी ख़राब हालत है.
फिल्म जिस पृष्ठभूमि पर बनी है वहाँ सूखा बहुत आम बात है, वैसे भी बुन्देलखण्ड में औसत से कम ही बारिश होती है. फिल्म में 'संजय मिश्रा' जिस एरिया में रहते हुए दिखाए गए हैं, बुंदेलखंड के बच्चे तो यह भी नहीं जानते कि मौमस के कई रंग होते हैं. बल्कि मौसम चार होते हैं. बच्चे सिर्फ दो मौसम ही जानते हैं सर्दी और गर्मी, बरसात के नाम पर तो बच्चों को बस इतना याद है कि कभी कभार एक दो दिन के लिए बारिश हो जाती है. बुंदेलखंड के लोगों एवं किसानों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण पानी ही है.
बुंदेलखंड के लोगों के लिए हवा भी कड़वी हो चुकी है, उन्हें अब हवा भी अज़ीब लगती है. फिल्म अनोखे तरीके से हमारे देश की जलवायु के विविध रंग दिखाती है. बैंक के कर्मचारी की भूमिका में 'रणवीर शौरी' वसूली के लिए बुंदेलखंड में उड़ीसा से आए हैं. मौसम विभाग की चेतावनी कहती है कि बढ़ता हुआ जलस्तर उड़ीसा के लिए इतना बड़ा खतरा है, कि उड़ीसा के कई शहर बढ़ते हुए जलस्तर से संकट के मुहाने पर हैं. जबकि बुंदेलखंड में पानी को तरसते हुए किसान हैं. बैंक अधिकारी गांव के अंधे बुजुर्ग से समझौता करता है कि अगर आप गांव में बैंक का कर्जा वसूलने में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका कर्ज़ मुआफ करवा दूँगा. और जल्दी से कर्ज वसूलने का कारण यह भी है कि बैंक अधिकारी जल्दी से अपने परिवार को यहां लाना चाहता है कि वो बढ़ते हुए जलस्तर में फंसे हुए परिवार को बचा सके. वहीँ अंधा बुजुर्ग इस टास्क को पूरा करने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है कि वो कर्ज के बोझ तले अपने बेटे को समाप्त नहीं होने देना चाहता.
फिल्म की कहानी इतनी सरल नहीं है कि कोई भी देख ले, इसके लिए कठोर हृदय चाहिए. आख़िरकार बैंक अधिकारी एवं बुजुर्ग अंधा किसान बैंक कर्ज वसूलने में नाकाम रह जाते हैं. नतीजतन बुजुर्ग का बेटा एक दिन गायब हो जाता है, और बैंक अधिकारी के परिवार वाले भी वहाँ फंसे रह जाते हैं. फिल्म आख़िरकार अपने सब्जेक्ट को सफ़लतापूर्वक दिखाने में सफ़ल तो हो जाती है लेकिन कई कचोटने वाले सवाल कर जाती है. ऐसे सवाल जो किसानों की पेशानी की झुर्रियों में स्पष्ट दिखते हैं, हालांकि हमारे सिस्टम को क्या ही गरज़ है कि वो किसानों की पेशानियों को पढ़े. ऐसी फ़िल्में बनाने के लिए जोखिम कहना इसलिए भी उचित है कि इनका ज्यादा जिक्र नहीं होता.
*कृषि प्रधान देश का सिनेमा किसानों के साथ नहीं दिखता*
---------------------------------------------------------------------
जी हां सिनेमा समाज का आईना कहा जाता है लेकिन जब बात सिनेमा में किसानो के दिखाने की बात आती है तो उस आईने में धूल दिखाई देती है. मेरा मानना है कि सिनेमा जिस तरह से समाज पर प्रभाव छोड़ता है, उस तरह तो साहित्य भी नहीं कर पाता, चूंकि देखने का अपना व्यापक असर होता है. देखा जाए तो जय जवान जय किसान का नारा देश में किसान एवं जवान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दिया गया था. जवानों के प्रति समाज में एक आदर का भाव है, अगर इसमे देखा जाए तो सिनेमा की भूमिका सबसे अग्रणी है. सिनेमा ने देश के आम जनमानस को बताया कि देश में सेना का क्या महत्व होना चाहिए. वहीँ किसानों पर यही सिनेमा की बेरुखी हैरतअंगेज है. अगर सिनेमा में किसानो को दिखाया जाता तो देश के अन्नदाता देश के जवानों की तरह आदर प्राप्त करते जिसके हकदार हैं. महान साहित्यकार मुन्शी प्रेमचंद ने लिखा है कि जिस देश में अधिकांश लोग कृषि पर गुजारा करते हों वहाँ के युवाओं को गोबर से बदबू आती है वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता. जिस देश में अधिकांश लोगों को गेंहू, धान, जौ... एवं सौंफ, जीरा अजवाइन में फर्क़ नहीं पता, जिन लोगों को यह नहीं पता कि दूध कितनी मेहनत से निकलता है. जिन्हें यह नहीं पता कि कौन सी फ़सल ज़मीन के अंदर से उगती है, कौन सी फसल पौधों से पैदा की जाती है, शहरों का एलीट क्लास का क्रूर रवैय्या देखिए. जब किसानों ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलन्द की तो उन्हें खालिस्तानी कहा गया इस बात पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के अन्नदाता के लिए लोगों के मन में कितना आदर का भाव है. जब तक इस देश का अन्नदाता मज़बूरी का जीवन जिएगा तब तक इस देश में खुशहाली नहीं आ सकती. रहा सवाल हिन्दी सिनेमा का तो ये सवाल तब तक और बड़े होते जाएंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना ही नहीं है.
दिलीप कुमार पाठक
फ़िल्म समीक्षक /पत्रकार
नई दिल्ली
फोन :
मेल : dileeppathak449@gmail.com



















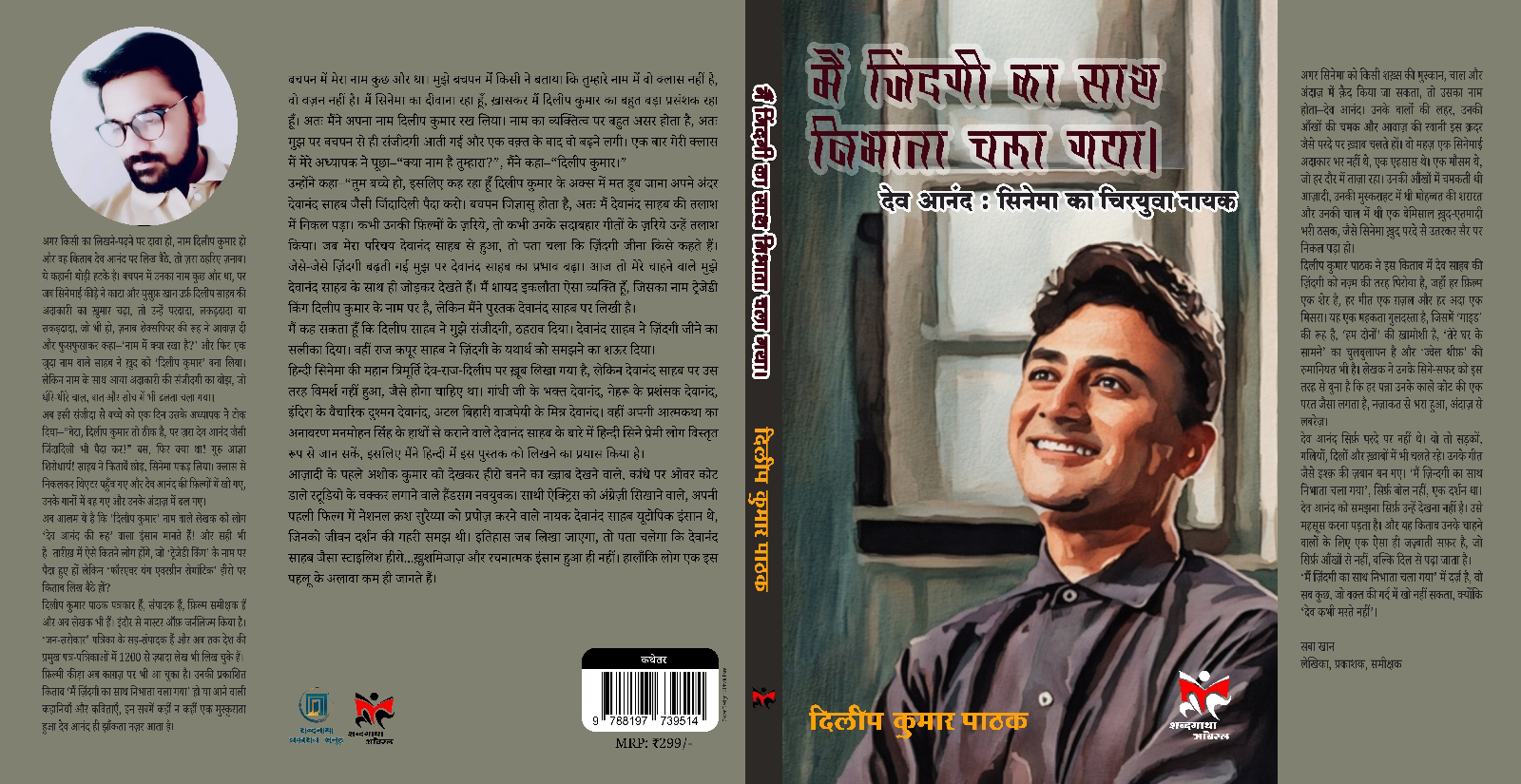


Comments
Post a Comment