(कविराज शैलेन्द्र)
साहित्य एवं गीतों की दुनिया के अनोखे राजकुमार
(कविराज शैलेन्द्र)
हिन्दी सिनेमा में गीतों का चाँद, जो गीतकारों में खुद एक आसमाँ था. जिसकी कलम से दहकते शोले निकलते थे. जिसकी तपिश से निरंकुश सत्ता का गुरुर जल कर मिट्टी में मिला देने की कुव्वत... वहीँ रूठी प्रेमिका को तारो के बीच से चाँद तोड़कर ले आने का प्रेम,व्यक्त करते उनके नग्मे...साफ़गोई ऐसी जिसने ग्रेट शो मैन राजकपूर को कह दिया, मैं पैसे के लिए नहीं लिखता में समाज के मुद्दो को तरजीह देता हूं. मेरी कविता बिकाऊ नहीं है. यह कहने का जज़्बा निडर, महान गीतकार शैलेन्द्र जैसी शख्सियत के साथ मेल खाता है. कविराज के कलम की ऐसी ताक़त की हिन्दी सिनेमा के क्या संगीतकार, क्या गीतकार, क्या निर्देशक, क्या निर्माता बड़े - बड़े दिग्गज उनके हुज़ूर में सजदा करते हैं. भूख एवं उसकी पीड़ा को बेबाक साफ़गोई से बयां करना, मुफलिसी, तंगहाली में जब घर में चूल्हा जलता है, तो उसकी आंच चाँद सी शीतलता प्रदान करती है, वहीँ आभाव में गुस्से से धधकती ज्वाला, सूरज को भी जलाकर राख कर दे. भूख एवं प्यास की तड़प ऐसी कि पेट और पीठ में फर्क़ खत्म हो जाए. भूख सहते हुए ज़िन्दगी जीने की चाहत और बढ़ जाए. ज़िन्दगी की आख़िरी साँस तक अपनी सृजनात्मक सोच, कल्पनाओं, आदि से ऐसे गीत, रचे.... शैलेन्द्र जी के गीतों का संसार इतना विस्तृत है, न शुरुआत है और न ही अंत.
कविराज शैलेन्द्र जी का जन्म 23 अगस्त 1923 को अविभाजित रावलपिंडी में हुआ था. इनका पूरा नाम शंकरदास केसरीलाल शैलेन्द्र था. शैलेन्द्र का पूरा परिवार भारत विभाजन के बाद भारत आ गया. मथुरा को अपना ठिकाना बनाया, तब कविराज शैलेन्द्र किशोर अवस्था में थे, कविराज अव्वल दर्जे के मेधावी छात्र थे. कक्षा 12 वीं में उत्तरप्रदेश में तीसरे स्थान पर आए. कविराज के पूर्वज बिहार से संबधित थे. प्रतिभा के साथ नियति की भी भूमिका होती है, कविराज अगर पेशेवर साहित्यकार न होते तो यकीन हॉकी के खिलाड़ी होते, लेकिन जो होना होता है, वही होता है. एक बार मैच के दौरान प्रतिद्वंद्वी टीम के एक खिलाड़ी ने शैलेन्द्र जी को एक जाति सूचक गाली दी, बगावती तेवर वाले कविराज चूंकि वो अपनी प्रतिभा या, अपने शब्दों से जवाब देना जानते थे, कलम के बाद हॉकी की स्टिक से सबसे ज्यादा मुहब्बत करने वाले कविराज ने अपनी जांघ पर मारकर तोड़ कर विरोध दर्ज कराया. शैलेन्द्र जी सुलझे हुए इंसान थे, वर्ना वो स्टिक उस अभद्र खिलाड़ी के भी मार सकते थे. उस वक़्त वो 17 साल के थे. गरीबी के कारण इलाज के आभाव में उनकी माँ एवं बहिन को असमय मौत ने मार डाला. गरीबी ने जीवन की जद्दोजहद के लिए घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे. आखिरकार शंकर दास केसरीलाल शैलेन्द्र घर से हिजरत कर गए. शंकर दास केसरीलाल जीविकोपार्जन के लिए मुंबई में रेल्वे की नौकरी की. प्रतिभा परिस्थितियों की गुलाम नहीं होती. रचनात्मकता कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती. यह हज़ारों में किसी एक को चुनती है. शैलेन्द्र जी ने विषम परिस्थितियों में भी कविताओं को लिखना जारी रखा. यूँ तो उन्होंने कविताएं बहुत पहले से ही लिखना शुरू किया दिया था. बंबई के कारखानों के शोर में कविताओं का सृजन इतना आसान नहीं था. नजदीकी लोग ताने मारते थे, कविताएं छोड़ो, कुछ काम करो कविताओं से पेट नहीं भरता. कविताएं भूखे पेट को रोटी नहीं देतीं सब भरे पेट के चोंचले हैं. शंकर दास से शैलेन्द्र बन चुके कविराज ने मजदूरों को बहुत नजदीक से देखा. रेल्वे एवं कारखानों में मजदूरों के साथ रहते हुए उनकी जरूरतों को समझा एवं ज़िन्दगी को इतने नजदीक से देखा, कि वो भाव बाद में उनकी कविताओं में साफ - साफ झाँकता था. शैलेन्द्र स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े, अपने शब्दों के जरिए अँग्रेजी सत्ता के विरुद्ध गीत लिखते थे. आजादी के बाद भी वो सवाल करते रहे, उनके लिए सत्ता एक जैसी ही होती है. कविराज विद्वता में तो महान ही थे, चौदह भाषा के जानकार, हिन्दी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, सहित चौदह भाषाएं सीखी, उनकी व्याकरण सीखी, भाषायी रूप से इतने समृद्ध हो चुके थे. आजादी के पहले ही जाने पहिचाने नाम थे.
शैलेन्द्र जी यूँ तो दिल से भावनात्मक थे, लेकिन विचारो से वामपंथी, अपने मिज़ाज से बगावती थे. शैलेन्द्र जी केवल गीतकारों की फ़ेहरिस्त तक सीमित नहीं थे, अपने लेखनी से देश को इंकलाब का ख्वाब दिखाने वालों की आवाज़ बन गए,जो जीत - हार से हटकर संघर्ष, मेहनत पर यकीन रखता था. सकारात्मक भाव उकेरने वाले कविराज लिखते हैं...
"तू ज़िन्दा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर,
अगर है कहीं स्वर्ग, तो उतार ला जमीन पर
ये ग़म के और चार दिन, सितम के और चार दिन
ये दिन भी गुज़र जाएंगे, गुज़र गए हज़ार दिन"
शैलेन्द्र जी ने काम करने वाले मजदूरों, के लिए ऐसा साहसिक नारा दिया, उस नारे ने निरंकुश सत्ता की जड़ें हिल गई. अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने अँग्रेजी सत्ता से तीखे सवाल किए सवालों से ब्रिटानिया सत्ता की चूलें हिल जाती थीं. देश आजाद हो जाने के बाद भी यही अंदाज़ कायम रहा, अँग्रेजी सत्ता, एवं आज़ाद भारतीय सत्ता में कोई ज्यादा फर्क़ नहीं है,सत्ता हर काल में एक जैसी होती है. विरोध के स्वर सहने का माद्दा नहीं होता, तब हर सत्ता दमनकारी नीति पर चलती है. साहित्यकारों को सत्ता की चरण चाशनी नहीं करना चाहिए. साहित्यकार को सत्ता से हमेशा बेहतरी के लिए आलोचना करते हुए सवाल करना चाहिए. जैसे ही साहित्यकार सत्ता से सवाल करना बंद कर देते हैं, सत्ता निरंकुश हो जाती है. समाज का निर्माण भी उसी स्तर पर होता है. शैलेन्द्र जी की प्रतिभा का आलम ऐसा, कि फिल्म फेयर के मंच से रूहानी गीतकार साहिर लुधियानवी साहब ने कहा था, "यह फिल्म फेयर मेरे गीत को नहीं इस सम्मान के हक़दार कविराज हैं. यह अवार्ड उन्हें ही मिलना चाहिए,क्योंकि उन्होंने मुझसे कहीं अच्छा गीत रचा है. यूँ तो शैलेन्द्र जी ने अपने पूरे कैरियर में केवल एक ही फिल्म 'तीसरी कसम' बनाई. जिसे निर्माता, कथाकार ख्वाजा अब्बास ने कहा था "यह फिल्म एक कविता की तरह है". हिन्दी सिनेमा को अपना आख़िरी गीत लिखकर दिया, उस गीत का भावार्थ समझाने के लिए शायद शैलेन्द्र जी ही समझा सकते थे, वर्ना आज भी उस गीत को समझना समुन्दर की लहरें गिनने के समान है, उस गीत के बोल हैं "जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहाँ".
कविराज महान गीतकार जिन्होंने हिन्दी सिनेमा में आते ही, प्रेम, रोमांस, की रूमानियत का ऐसा जादू चलाया, कि आज भी कोई उस तिलिस्म से बाहर नहीं आ सका. उनके गीतों की ऐसी मिठास की आज भी उसकी मिठास की अनुभूति होती है. शैलेन्द्र जी ही वो गीतकार हैं, जिन्होंने हिन्दी सिनेमा को पहला कैबरे गीत लिखा. शैलेन्द्र जी केवल क्रांति के भावों के साथ - साथ रिश्तों के ज़ज्बात सुनकर आजादी के बाद की चार पांच पीढ़ियां बड़ी हुईं. कविराज ने बच्चों के लिए अपने प्यार को उसकी कोमलता को अपने शब्दों से लिखा. दादी - नानी, अपने बुजुर्गों के लिए बच्चों के भावों को उकेरने वाले गीत भी हम गुनगुनाने लगते हैं. कविराज बच्चों को देश का भविष्य मानते थे, उनका मानना था, कि हम सब को बच्चों के इर्द - गिर्द ख्वाबों की ताबीर गढ़ना चाहिए. कविराज ने भी आसान शब्दों में बच्चों के लिए भी कालजयी गीत लिखे. भाई - बहिन के प्यार की मर्यादा, बेटियों के माँ बाप के लिए क्या भाव होते हैं, उनको बहुत ही सुन्दर मार्मिक शब्दों में गीत रचे. कविराज के गानों में लोकगीतों एवं संस्कृति की मिठास का समावेश, आंचलिकता की खुशनुमा भाव एवं उसकी रूमानियत अपनेपन का एहसास करा देते थे. आंचलिकता एवं लोकगीतों, संस्कृति से सुसज्जित कविराज शैलेन्द्र जी का हर गीत यादगार है. हर गीत के रचे जाने का अपना एक किस्सा है, उसका अपना मह्त्व प्रासंगिक है. कविराज के गीतों में स्त्री वेदना, भावनाओं की भीनी फुहार, आम जनमानस का सरोकार, लोकगीतों सहित उसकी महक, स्त्री विमर्श से स्त्रियों के लिए कुछ निकलती समाज में गुंजाइशें कुछ निकल कर आईं. दुःख दर्द में भी ज़िन्दगी जीने का ढंग यूँ ही नहीं उन्होंने उकेरा इससे जुड़ा उनका बचपन, किशोरावस्था, दो जून की रोटी की जद्दोजहद में अपने साहित्य एव मूल्यों को बचाने के बाद के भाव थे. जो कभी गुस्सा, कभी दुःख, दर्द, और कभी न खत्म होने वाला प्रेम छलकता था.
शैलेन्द्र के लिए साहित्यकार, कहानीकार, भीष्म साहनी कहते थे " हिन्दी सिनेमा में शैलेन्द्र के आने के बाद से जो सबसे बड़ा बदलाव आया,वो था, आम आदमी के सरोकार हिन्दी सिनेमा के गीतों में दिखने लगे थे"उनके गीतों में तेवर ही अलग थे, बेबाक चुनौतीपूर्ण आवाज़, जिसमें दृढ़ता थी ". साहित्यकार शैलेन्द्र का गीतकार बनना उनके गीतों के समान ही बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रक्रिया है. शैलेन्द्र जी के गीतों की ख़ासियत थी, कि बड़ी से बड़ी बातों को सरल सहज शव्दों का ऐसा तानाबाना बुनते थे, लेकिन उनके गीतों की तरह उनका हिन्दी सिनेमा में जाना इतना सरल नहीं था. वो फ़िल्मों के गीत लिखेंगे,क्योंकि अपनी क्रांति की पहिचान के साथ खूब प्रसिद्ध थे.
राज कपूर सन 1947 में फिल्म 'आग' बना रहे थे. उसी समय पृथ्वी थियेटर के सामने जनवादी लेखक संघ का आंदोलन हुआ था. उसमे शैलेन्द्र भी एक कवि के रूप में सदारत फर्मा रहे थे, तब ही राज कपूर एवं पृथ्वीराज कपूर ने उनको सुना. कविराज "जलता है पंजाब" नामक कविता पढ़ रहे थे, पंजाबी पृष्ठभूमि से उपजे कपूर खानदान के ग्रेट शो मैन राज कपूर साहब इस कविता से खूब प्रभावित हुए. राज कपूर साहब ने शैलेन्द्र जी से कहा मैं एक आग नामक फिल्म बना रहा हूं, अगर आप उचित समझे क्या आप मेरी फिल्म के गीत लिखेंगे, क्या आप मुझे आप अपनी कविताएं देंगे. शैलेन्द्र जी सरोकार के लिए लिखते थे. उन्होंने जो राज कपूर को जवाब दिया उसके लिए दिलेर कलेजा चाहिए. अतः उन्होंने राज कपूर को कहा कि मैं पैसे के लिए नहीं लिखता, मेरी कविता बिकाऊ नहीं है. राज कपूर थोड़ा सुनकर नाराज हुए, लेकिन कुछ व्यक्त नहीं किया, उन्होंने अपने घर का पता शैलेन्द्र जी को दे दिया, कहा " शैलेन्द्र जी आपको कभी भी मेरी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो ज़रूर याद कीजिएगा".ऐसा कहकर राज कपूर चले गए. क्रांतिकारी कवि शैलेन्द्र एवं राज कपूर दोनों की पहली तल्ख मुलाक़ात में राज कपूर की विनम्रता ने दोनों की दोस्ती का एक युग शुरू करने का एक अध्याय लिख चुके थे. अंजाम तक पहुंचाने के लिए शैलेन्द्र के हाथो छोड़ आए.
राज कपूर जिस काग़ज़ के टुकड़े पर अपना पता दे गए थे, वो एक युग को शुरू करने का पूरा का पूरा दस्तावेज था. दोनों अपनी - अपनी ज़िन्दगी में मुब्तिला हो गए. आख़िरकार समय ने फिजा बदली, शैलेन्द्र अपने निजी जीवन में संघर्ष कर रहे थे, ग्रेट शो मैन राज कपूर साहब बरसात फिल्म बना रहे थे. उसी दिनों शैलेन्द्र की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गईं, हस्पताल में भर्ती होना पड़ा. पत्नी के इलाज के लिए पैसे की जरूरत हुई, पत्नी की हालत खराब एवं उनके संघर्ष के साथ, राज कपूर की विनम्रता याद आई अतः कविराज उनके घर गए. अपनी आवश्यकता बताते हुए राज कपूर से पांच सौ रुपये उधार माँगा. उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी, राज कपूर ने उनकी मदद की और पांच सौ रुपये सहर्ष दे दिया. शैलेन्द्र इस पैसे को वापस करने के वादे को पूरा करने के बाद चले गए. समय गुजरने के बाद राज कपूर के पैसे वापस करने के लिए उनके घर जाते हैं. यही से शैलेन्द्र एवं राज कपूर के रिश्ते की शुरुआत होती है. राज कपूर ने पहली मुलाकात को याद किया. उनके स्वभाव को देखते हुए विनम्रता से पैसे लेने से मना कर दिया. कविराज की भावनाएं आहत न हों, इस बात का ख्याल रखते हुए, फिल्म बरसात के गीत लिखने की गुजारिश किया. उस समय कुछ राज कपूर की विनम्रता एवं समय की मांग थी, यही से शरू होती है अंतिम साँस तक चलने वाली दोस्ती जो शैलेन्द्र एवं राज कपूर दोनों के बीच रही. बारसात फिल्म से ही हसरत जयपुरी, शंकर - जय किशनजी आदि भी जुड़े जो अपने फिल्मी कॅरियर की शुरुआत कर रहे थे. जिनका अनोखा ग्रुप बना जो सत्रह साल तक सफ़लता को नेपथ्य में ले जाने में शैलेन्द्र जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही. इस महत्वपूर्ण सफर में कविराज ने जीवन के हर रंग में गीत लिखे. गीतों साहित्यकारों में उस दौर में इतनी विद्वता, इतनी विविधता, सिर्फ शैलेन्द्र मे थी. गोल्डन एरा में गीतकारों की चौकड़ी का अहम हिस्सा... मजरुह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूंनी तीनों के साथ कविराज शैलेन्द्र जी का नाम सर्वश्रेष्ठ गीतकारों में शुमार था. बरसात फिल्म से मेरा नाम जोकर तक शैलेन्द्र जी की अंतिम साँस तक साथ रहा. दोनों के रिश्तों की डोर दोनों के हाथो में थी. नयी प्रतिभा को पहिचान लेने की कला एवं विद्वता का ऐसा संगम जो दोनों एक - एक सिरे को थामे हुए थे. कविराज ने अपनी कलम से ऐसे गीत रचे कि रूपहले पर्दे की शोहरत सातवे आसमान में थी. क्लासिकल फ़िल्मों के दौर में राज कपूर के लिए उन्होंने आवारा, बूट पोलिश, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, अनाड़ी, तीसरी कसम, अब दिल्ली दूर नहीं जैसी महानतम फ़िल्मों में यथार्थ गीत लिखे जिसे शंकर - जय किशनजी ने अपने संगीत से सजाया. वहीँ राज कपूर साहब ने अपने भोलेपन, सादगी से पर्दे पर उकेरा कि शैलेन्द्र जी को महसूस किया जा सकता है. हिन्दी सिनेमा को सातवें आसमान पर पहुचाने वाले निर्माता / निर्देशकों की पहली पसंद थे. जिसमें हिन्दी साहित्य को हिन्दी सिनेमा में लेकर आने वाले दूरदर्शी निर्देशक विमल रॉय, देवानंद साहब, महान संगीतकार बर्मन दादा, आदि के साथ काम करते हुए, दो बीघा ज़मीन, बसंत बहार, बंदिनी, गाइड, यहूदी, दिल अपना प्रीत पराई, मुनीम जी, छोटी बहिन, जंगली, पतीता, काला बाज़ार, जानवर, सीमा, ब्रम्हचारी, जैसी महान फ़िल्मों में कभी न भुलाए जाने वाले कालजयी गीत लिखे. जो आज भी प्रासंगिक हैं. कविराज के गीतों में आम जीवन बहता था, आम आदमी का सरोकार देखा जा सकता है.
गीतकार शैलेन्द्र ने आम आदमी के सरोकार को व्यावसायिक सिनेमा से जोड़ दिया. शब्दों का भाव ऐसा संतुलन की सरोकार एवं व्यपारिक दोनों के मूल्य बचे रहें. शैलेन्द्र जी जैसी शख्सियत किसी भी क्षेत्र में युगों में पैदा होते हैं, और रच जाते हैं पूरा का पूरा गीतों का संसार...
शैलेन्द्र जी ने भारतीय सिनेमा के लिए नायाब तोहफ़ा देकर गए. उन्होंने अपनी सिनेमाई समझ दिखाते हुए, "तीसरी कसम" जैसी महान कल्ट फिल्म का निर्माण कर दिया. 'तीसरी कसम' को एक साल में बन जाना चाहिए था, लेकिन फिल्म का निर्माण चार साल तक होता रहा, किसी ने डेट्स नहीं दिए, किसी ने पूरा सहयोग नहीं दिया. फिल्म के निर्माण में शैलेन्द्र जी अकेले पड़ते जा रहे थे, शैलेन्द्र जी ने इस फिल्म में अपनी पूरी हस्ती लगा दी थी. शैलेन्द्र जी ने जितनी शिद्दत से फिल्म बनाई, उस तरह फिल्म को सफलता नहीं मिली. फिल्म की असफ़लता ने शैलेन्द्र जी को तोड़कर रख दिया. कविराज ने फिल्मी दुनिया का सच समझ चुके थे, अंततः उन्होंने कसम खाई, कि अब कभी फ़िल्मों का निर्माण नहीं करेंगे. शैलेन्द्र जी जिस मिट्टी के बने थे, उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता था, लेकिन हिन्दी सिनेमा के सच को स्वीकार करते हुए अपनी कलम से इस सच को साधना ही नहीं चाहते थे. पैसों के नुमाइंदों के लिए शैलेन्द्र जी की पर्सनैलिटी को तोड़ पाना इतना आसान नहीं था. पैसे के पुतलों के सामने शब्दों का एक ऐसा महारथी खड़ा था. शैलेन्द्र जी खुद के सामने सरोकार को मरते हुए नहीं देख सकते थे, जिन्होंने अपने कंधे पर उठा रखा था. आख़िरकार शैलेन्द्र जी 13 दिसंबर को हस्पताल में भर्ती हुए, इस उम्मीद के साथ कि फिर से लौटकर हिन्दी सिनेमा को अपनी कलम से सीचेंगे, लेकिन नियति अपना दांव चल चुकी थी, शायद ऊपर वाले को किसी जिंदादिल लेखक की जरूरत रही होगी. अंततः 14 दिसम्बर 1966 को शैलेन्द्र जी इस फानी दुनिया से रुख़सत कर गए. दोनों महान विभूतियों को एक साथ ही याद किया जाता है. दोनों आत्माएं एक - दूसरे के बिना अधूरी हैं. शैलेन्द्र जी आज भी अपने गीतों के संसार में, आम लोगों के सरोकार में सत्ता को चुनौती देने वाले नारों में... बच्चों के गीतों में, शैलेन्द्र जी तब तक अजर - अमर रहेंगे, जब तक यह कायनात है... शैलेन्द्र जी को मेरा शत - शत प्रणाम.......
दिलीप कुमार









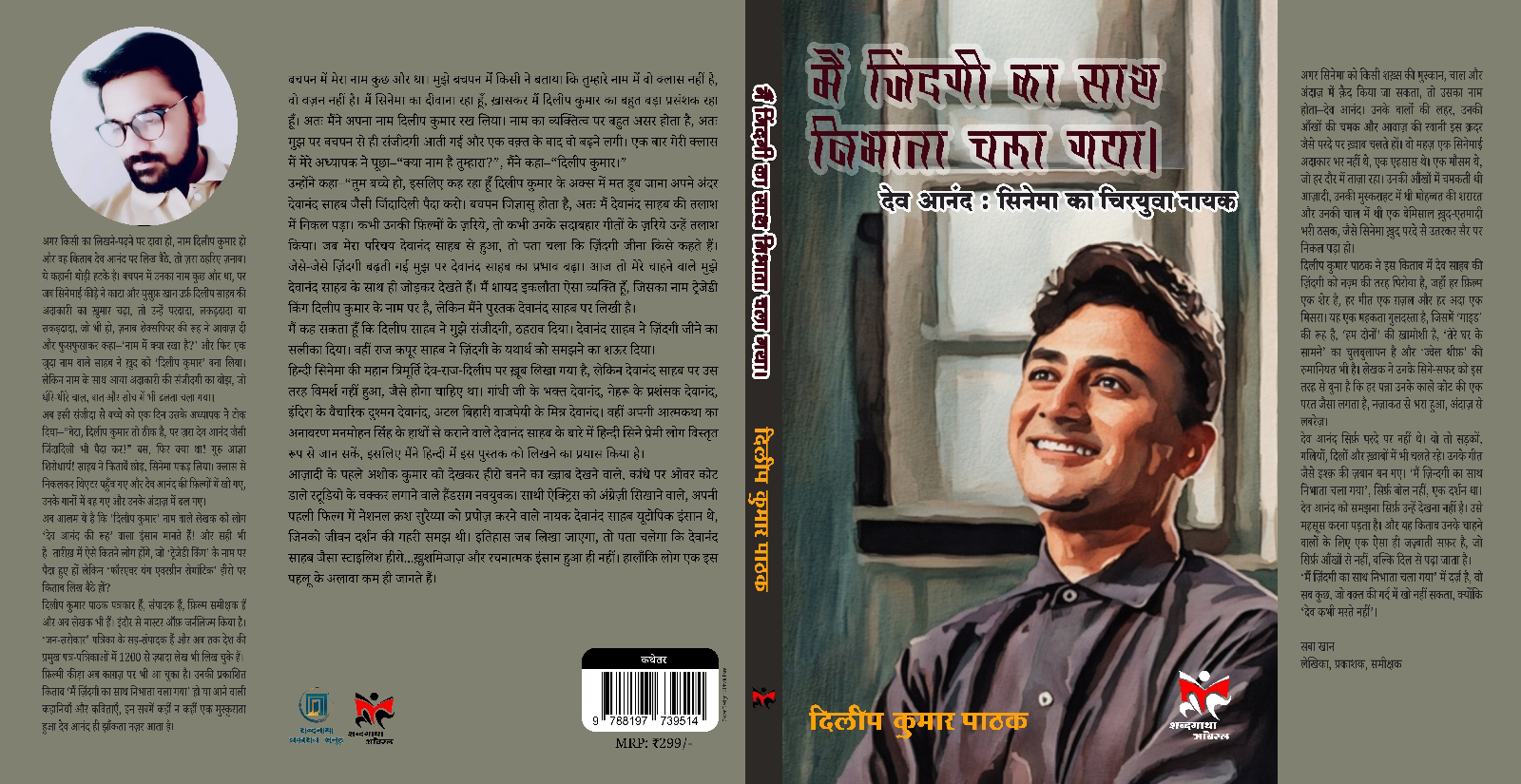

Comments
Post a Comment